3 अंकों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर
प्र.1. ‘प्रशस्ति’ क्या होती है? इसका एक उदाहरण दीजिए।
🔹 उत्तर:
- प्रशस्ति का अर्थ है “प्रशंसा करना” – ये ऐसे शिलालेख होते हैं जो शासकों की वीरता, दानशीलता और शक्तियों का बखान करते हैं।
- प्रशस्तियाँ आमतौर पर कवियों और दरबारी लेखकों द्वारा संस्कृत भाषा में रची जाती थीं।
- उदाहरण: इलाहाबाद स्तंभ लेख जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है, इसे हरिषेण ने लिखा था।
प्र.2. अशोक के ‘धम्म’ की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं?
🔹 उत्तर:
- धार्मिक सहिष्णुता – सभी धर्मों का सम्मान।
- नैतिक जीवन – माता-पिता का आदर, बड़ों का सम्मान, दया और करूणा।
- अहिंसा – हिंसा, पशुबलि और युद्ध के विरुद्ध।
- धम्म महामात्रों की नियुक्ति – धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारी।
प्र.3. गहपति कौन था? उसके क्या कार्य होते थे?
🔹 उत्तर:
- गहपति शब्द का अर्थ है गृहस्वामी या परिवार का मुखिया।
- यह किसान, शिल्पकार या व्यापारी भी हो सकता था।
- वह:
- खेती-बाड़ी का संचालन करता था।
- श्रमिकों का प्रबंध करता था।
- कर और उत्पाद का उत्तरदायी होता था।
प्र.4. मौर्य प्रशासन की दो विशेषताएँ लिखिए।
🔹 उत्तर:
- केंद्रीकृत शासन व्यवस्था – सम्राट का नियंत्रण पूरे साम्राज्य पर था। राजधानी पाटलिपुत्र से शासन चलता था।
- प्रशासनिक अधिकारी – सामाहर्ता (राजस्व अधिकारी), नगरक (नगर प्रमुख), अमात्य (सचिव) आदि नियुक्त होते थे।
प्र.5. अशोक के अभिलेखों की विशेषताएँ बताइए।
🔹 उत्तर:
- ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लिपि प्रायः ब्राह्मी या खरोष्ठी थी।
- ये पत्थर, स्तंभ और चट्टानों पर खुदे होते थे।
- इनमें अशोक के धम्म, नीतियाँ और सार्वजनिक घोषणाएँ शामिल हैं।
प्र.6. भूमि अनुदानों से समाज में क्या परिवर्तन हुए?
🔹 उत्तर:
- ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि मिलने से ब्राह्मणों की शक्ति में वृद्धि हुई।
- अनुदानित भूमि पर कर वसूली का अधिकार मिला – जिससे स्थानीय लोगों पर बोझ बढ़ा।
- विश्टि (बेगारी) प्रथा बढ़ी – श्रमिकों से मुफ्त में काम लिया जाने लगा।
प्र.7. पंच-चिह्नित सिक्कों की विशेषताएँ बताइए।
🔹 उत्तर:
- ये चाँदी या तांबे के होते थे।
- इन पर किसी राजा का नाम नहीं होता था, केवल प्रतीक/चिह्न होते थे (जैसे सूरज, पेड़)।
- व्यापारिक लेन-देन में इनका प्रयोग होता था – ये स्थानीय शासन या व्यापारी श्रेणियों द्वारा जारी होते थे।
प्र.8. ‘श्रेणि’ क्या थी? समाज में इसका क्या महत्व था?
🔹 उत्तर:
- श्रेणि एक प्रकार का व्यापारियों या कारीगरों का संघ था।
- ये:
- व्यापारिक हितों की रक्षा करती थीं।
- सदस्यता प्रदान करती थीं।
- सामूहिक कार्य जैसे दान, मठ निर्माण आदि में भाग लेती थीं।
प्र.9. मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे?
🔹 उत्तर:
- विशाल साम्राज्य का प्रबंधन कठिन था।
- शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी।
- उत्तराधिकारियों की कमजोरी और अक्षमता।
- अशोक की धम्म नीति से सैन्य शक्ति कमजोर हुई।
प्र.10. ब्राह्मी लिपि की खोज किसने की और इसका क्या महत्व है?
🔹 उत्तर:
- ब्राह्मी लिपि की पहचान 1837 में जेम्स प्रिन्सेप ने की थी।
- इसके माध्यम से:
- अशोक के अभिलेख पढ़े जा सके।
- प्राचीन भारत के इतिहास, शासन और समाज की जानकारी मिली।
- यह प्राचीन भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक आधार बनी।
8 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न 1. मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें।
(या)
प्रशासनिक प्रणाली की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य को एक संगठित साम्राज्य क्यों कहा जाता है?
उत्तर:
मौर्य साम्राज्य (321 ई.पू. – 185 ई.पू.) भारतीय उपमहाद्वीप का पहला केंद्रीकृत और विशाल साम्राज्य था। इसकी प्रशासनिक प्रणाली का वर्णन ‘अर्थशास्त्र’, ‘मेगस्थनीज़ की इंडिका’ और अशोक के अभिलेखों में मिलता है।
🔷 प्रमुख विशेषताएँ:
- केंद्रीकृत शासन व्यवस्था:
- राजा सर्वोच्च शासक होता था, जो न्याय, सेना, राजस्व आदि का नियंत्रण करता था।
- प्रशासनिक विभाजन:
- साम्राज्य को प्रांतों में बाँटा गया था। प्रांतपाल या राजकुमार (कुमार) इनका संचालन करते थे।
- प्रत्येक प्रांत को जिलों और गाँवों में बाँटा गया था।
- मुख्य अधिकारी:
- अमात्य – मंत्री/सचिव,
- समाहर्ता – कर संग्रहकर्ता,
- नगरक – नगरों का प्रमुख,
- धम्म महामात्र – अशोक द्वारा नियुक्त नैतिकता प्रचारक।
- सेना संगठन:
- विशाल सेना – पैदल, अश्व, हाथी, रथ।
- युद्ध और सुरक्षा का विस्तृत प्रबंध।
- गुप्तचर प्रणाली:
- गुप्तचर (जासूस) राजा को प्रत्येक गतिविधि की सूचना देते थे।
- दो प्रकार के जासूस – बाहरी व आंतरिक।
- राजस्व व्यवस्था:
- भूमि पर ‘भाग’ कर लिया जाता था (1/6 भाग)।
- अन्य कर: व्यापार, पशुपालन, शिल्प, सीमाशुल्क आदि।
- धम्म नीति (अशोककालीन):
- अशोक ने शासन में नैतिकता को जोड़ा।
- धम्म महामात्र नियुक्त कर जनता को धर्म, सहिष्णुता व सेवा का संदेश दिया।
📌 निष्कर्ष:
मौर्य शासन व्यवस्था प्राचीन भारत की एक आदर्श केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली थी। इसमें नियंत्रण, संगठन और दायित्व स्पष्ट थे।
✅ प्रश्न 2. अशोक के धम्म की विशेषताएँ बताइए। उसका उद्देश्य और प्रभाव स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
धम्म अशोक द्वारा स्थापित नैतिक आचार संहिता थी। यह किसी धर्म का प्रचार नहीं था, बल्कि सार्वजनिक नैतिकता और सदाचार का संदेश था।
🔷 धम्म की प्रमुख विशेषताएँ:
- धार्मिक सहिष्णुता:
- सभी धर्मों का सम्मान करें, आपसी वैमनस्य न रखें।
- नैतिक आचरण:
- माता-पिता का आदर, बड़ों का सम्मान, गुरु सेवा।
- अहिंसा और करूणा:
- पशु बलि का विरोध, सभी प्राणियों के प्रति दया।
- समाज सेवा:
- दास-दासियों, वृद्धों, श्रमिकों के साथ दया का व्यवहार।
- धम्म महामात्रों की नियुक्ति:
- धम्म के प्रचार के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- सार्वजनिक कार्य:
- यात्रियों हेतु कुएँ, सड़कें, वृक्ष, अस्पताल आदि का निर्माण।
🔷 उद्देश्य:
- विशाल साम्राज्य में एकता और सामाजिक शांति स्थापित करना।
- युद्धों से जनजीवन में उत्पन्न हिंसा और दुख को समाप्त करना।
🔷 प्रभाव:
- समाज में नैतिकता, सह-अस्तित्व और करुणा की भावना बढ़ी।
- अशोक को इतिहास में ‘भारत का पहला कल्याणकारी शासक’ माना गया।
📌 निष्कर्ष:
अशोक का धम्म उस युग की एक नवीन और व्यावहारिक सामाजिक नीति थी, जिसने शासन में नैतिक मूल्यों को जोड़ा।
✅ प्रश्न 3. भूमि अनुदान प्रणाली का विवरण दें। इससे समाज और प्रशासन में क्या परिवर्तन आए?
उत्तर:
भूमि अनुदान प्रणाली प्राचीन भारत में विशेष रूप से मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में प्रचलित हुई, जिसमें शासक ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को भूमि दान देते थे।
🔷 भूमि अनुदान की विशेषताएँ:
- अनुदान ताम्र पत्रों या शिलालेखों पर दर्ज होता था।
- दान में दी गई भूमि पर कर छूट होती थी।
- प्राप्तकर्ता को प्रशासनिक अधिकार भी मिलते थे – जैसे कर संग्रह, दंड देना, श्रम लेना (विश्टि)।
- दान स्थायी या उत्तराधिकार में देने योग्य होता था।
🔷 समाज पर प्रभाव:
- ब्राह्मणों और मंदिरों की आर्थिक शक्ति बढ़ी।
- ग्रामवासियों पर दबाव बढ़ा – अब वे दानदाता के अधीन हो गए।
- विश्टि (बेगारी) प्रथा बढ़ी – किसानों से जबरन श्रम लिया गया।
🔷 प्रशासन पर प्रभाव:
- राजा का सीधा नियंत्रण कम हुआ।
- स्थानीय स्तर पर स्वायत्तशासी ग्राम प्रणाली विकसित हुई।
- अनुदानों से धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं को संरक्षण मिला।
📌 निष्कर्ष:
भूमि अनुदान प्रणाली ने प्राचीन भारत के सामाजिक ढांचे और प्रशासनिक प्रणाली को गहराई से प्रभावित किया और वर्ण आधारित सत्ता संतुलन को मजबूत किया।
✅ प्रश्न 4. शहरीकरण की प्रक्रिया को प्राचीन भारत के साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर:
600 ई.पू. से 600 ई. के बीच भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ी। इस काल में व्यापार, कृषि और शासन के कारण कई नए नगर विकसित हुए।
🔷 प्रमुख साक्ष्य एवं बिंदु:
- नगरों का विकास:
- पाटलिपुत्र, मथुरा, उज्जैन, तक्षशिला आदि प्रमुख नगर।
- ये प्रशासन, शिल्पकला और व्यापार के केंद्र बने।
- संगठित नगरीय संरचना:
- नगरों में सड़कें, नालियाँ, बाजार, नगर रक्षा दीवारें आदि थीं।
- कारीगर और श्रेणियाँ:
- कारीगरों (लोहार, बढ़ई, बुनकर) और व्यापारियों की श्रेणियाँ (Guilds) थी।
- श्रेणियाँ श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा, मूल्य निर्धारण आदि में सहायता करती थीं।
- व्यापार और मुद्रा:
- पंच-चिह्नित सिक्कों, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं, और समुद्री व्यापार ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया।
- बंदरगाहों का महत्व:
- अरिकमेडु, भरूच, तम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े।
- साहित्यिक साक्ष्य:
- संगम साहित्य में नगरों, व्यापारियों और सामाजिक संरचना का वर्णन मिलता है।
📌 निष्कर्ष:
प्राचीन भारत का शहरीकरण एक जटिल परंतु जीवंत प्रक्रिया थी, जो राजनीतिक स्थिरता, कृषि अधिशेष और व्यापारिक गतिविधियों पर आधारित थी।



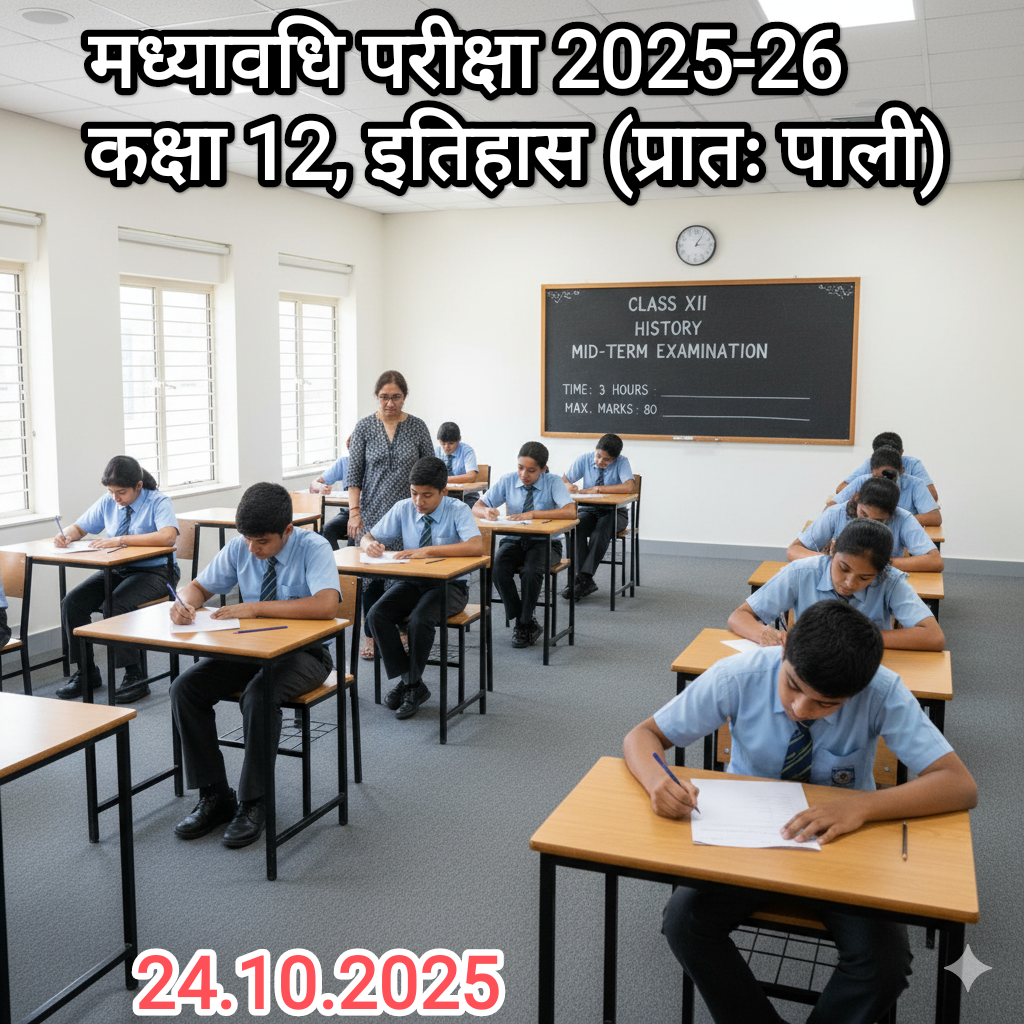
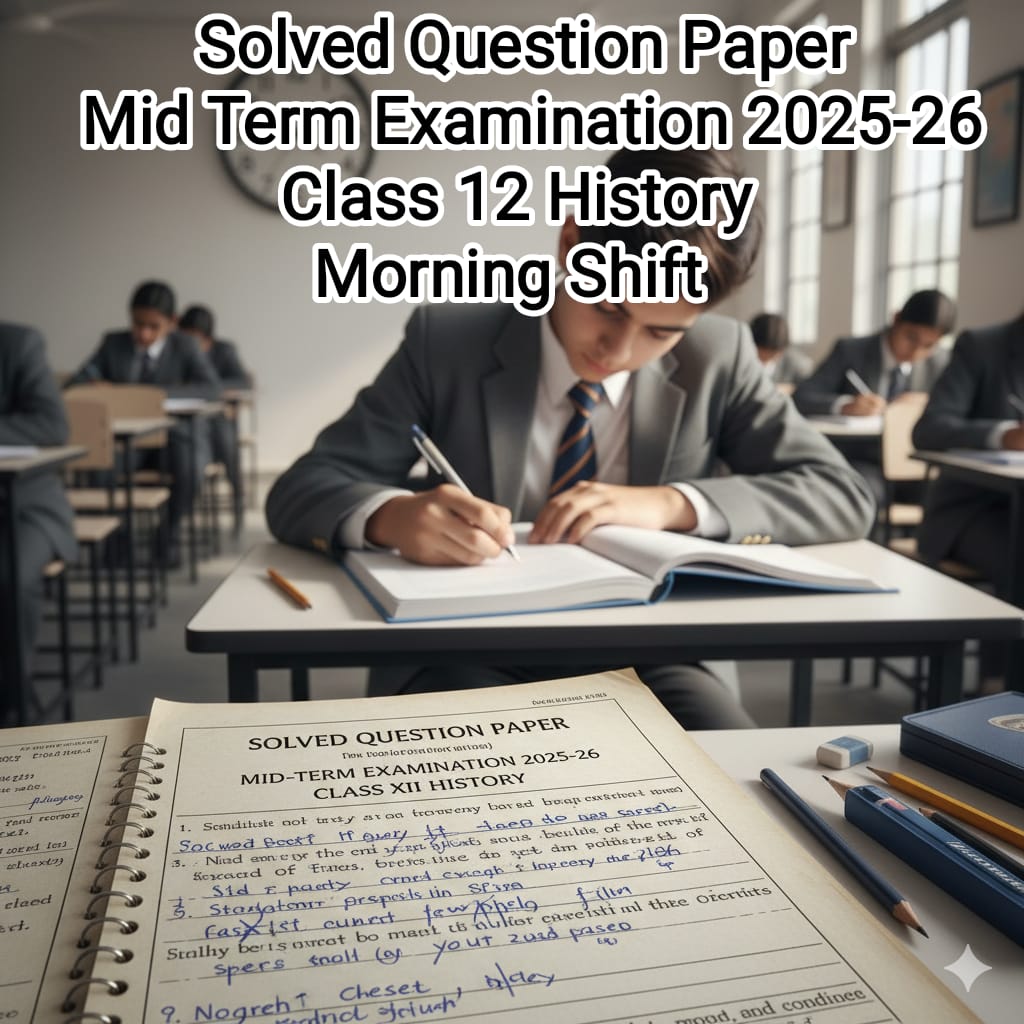
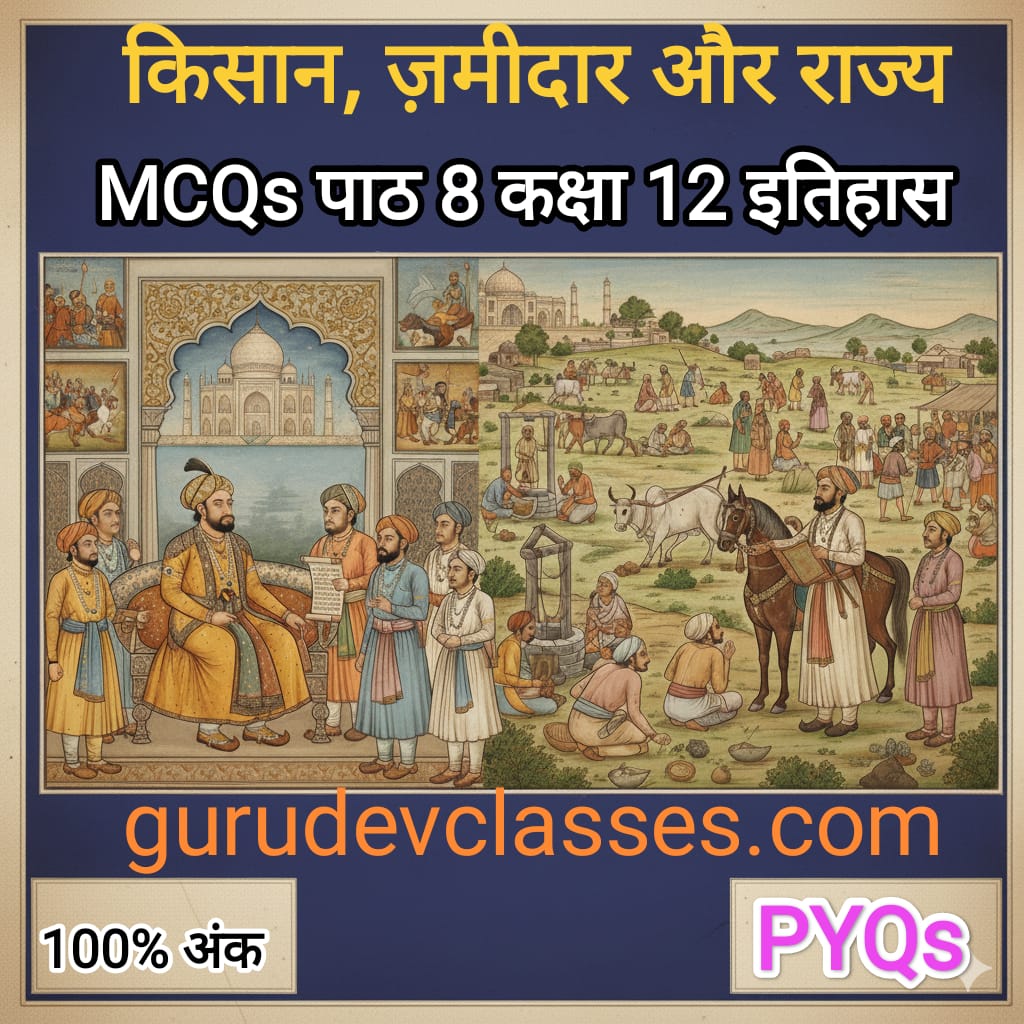

thank’s sir for providing this notes i am your student for class 12th B