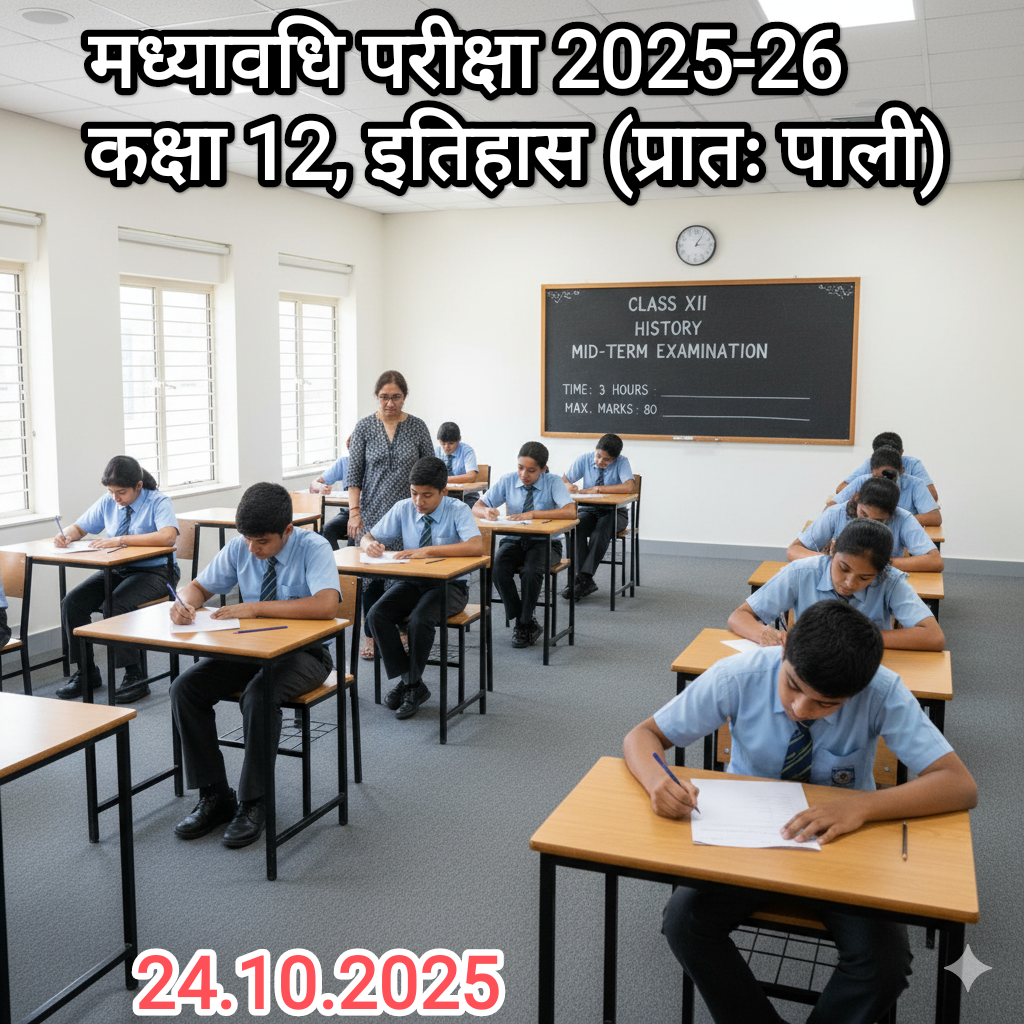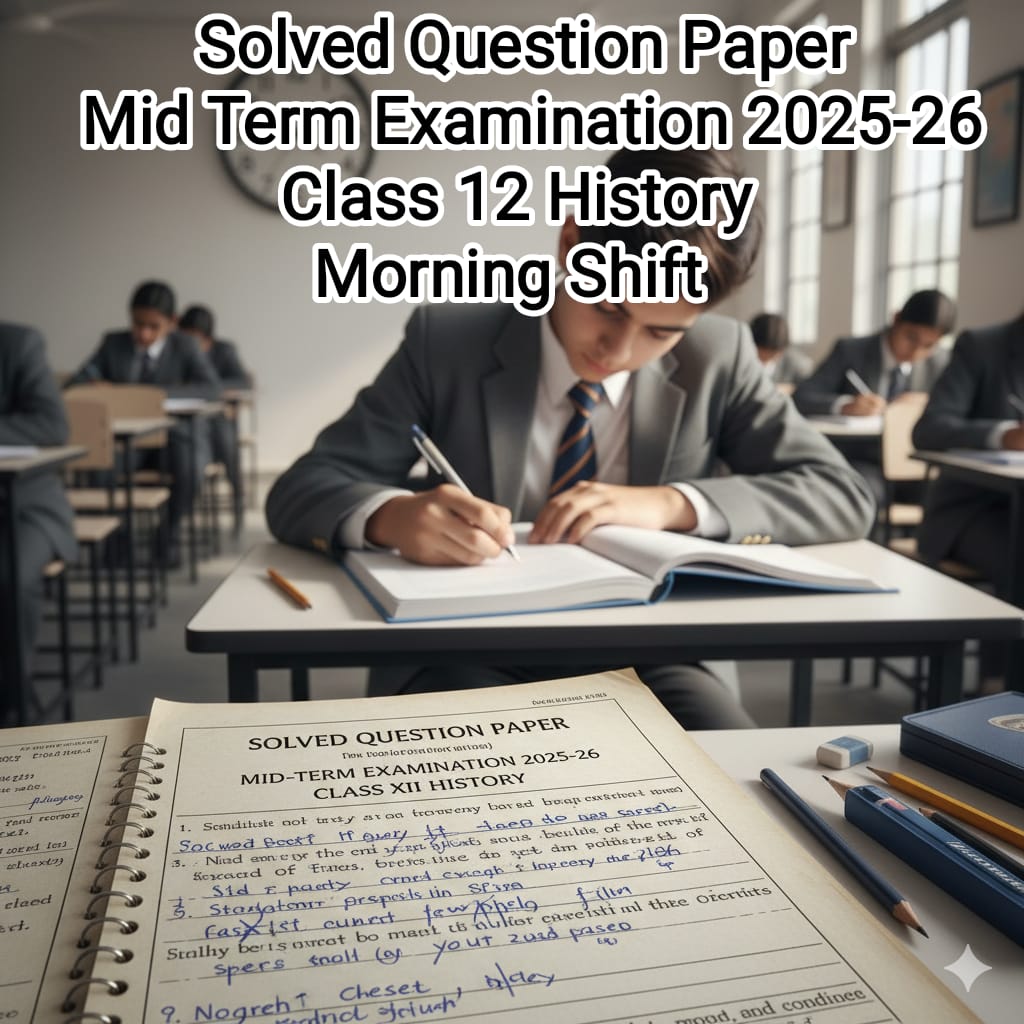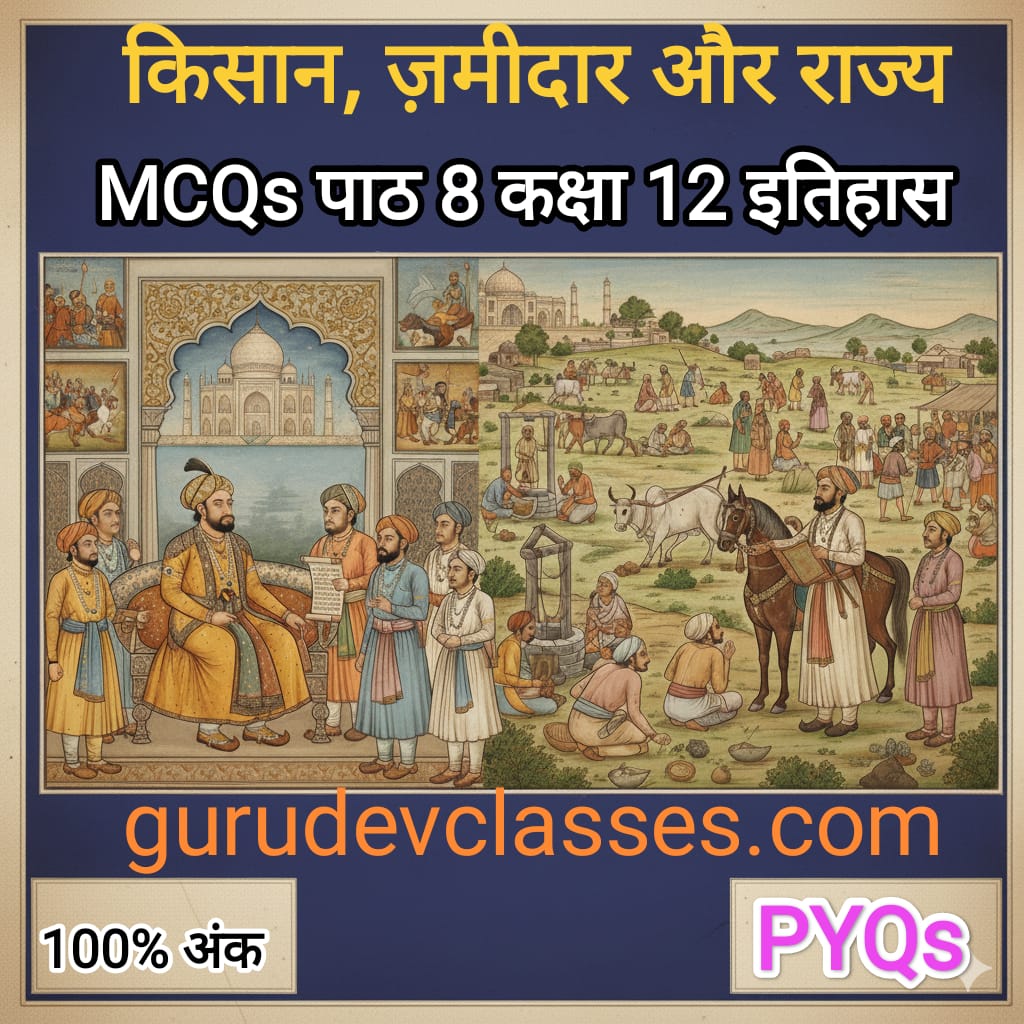कक्षा 12 इतिहास (Themes in Indian History – Part I)
🔷 भूमिका
- आठवीं से अठारहवीं शताब्दी के बीच भारत में धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं में बड़े बदलाव हुए।
- भक्ति और सूफ़ी परंपराएँ लोगों की आध्यात्मिक ज़रूरतों की अभिव्यक्ति बनकर उभरीं और परंपरागत ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी।
- इन आंदोलनों ने व्यक्तिगत भक्ति, सामाजिक समानता, और जातिवाद के विरोध पर ज़ोर दिया।
🧭 खंड I: धार्मिक विश्वासों और परंपराओं की पृष्ठभूमि
● भक्ति और सूफ़ी से पहले की धार्मिक स्थिति
- भारत में कई धार्मिक मान्यताएँ प्रचलित थीं: वैदिक, पुराणिक, बौद्ध, जैन, आदिवासी परंपराएँ, ग्राम देवता, पूर्वज पूजा आदि।
- प्रमुख देवता: विष्णु, शिव, दुर्गा – पूरे भारत में पूजे जाते थे।
- स्थानीय देवताओं की भी व्यापक मान्यता थी, जिन्हें धीरे-धीरे संस्कृतिकरण के माध्यम से ब्राह्मणिक परंपरा में शामिल किया गया।

● एक परम ईश्वर की धारणा
- ईस्वी सन् की शुरुआत के बाद एक परमात्मा या व्यक्तिगत ईश्वर की अवधारणा लोकप्रिय हुई।
- दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभरीं:
- सगुण भक्ति – साकार रूप में ईश्वर की भक्ति (राम, कृष्ण, शिव आदि)
- निर्गुण भक्ति – निराकार ईश्वर की भक्ति
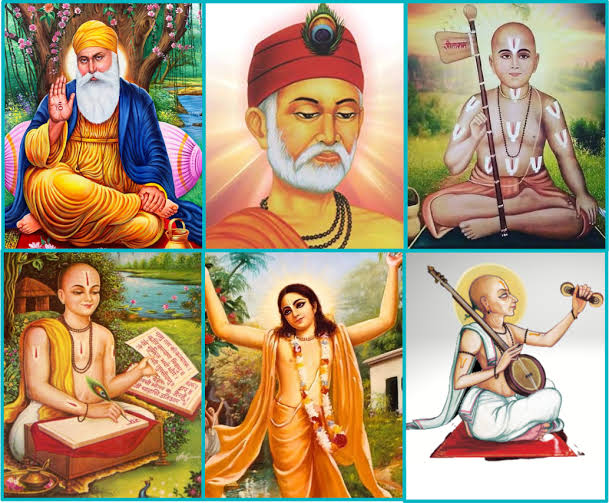
● तांत्रिक परंपराएँ
- तंत्र परंपराओं में मंत्र, साधना, और स्त्री शक्ति (शक्ति) की पूजा पर ज़ोर था।

- यह परंपराएँ हिन्दू, बौद्ध, जैन और मुस्लिम संतों में भी देखी गईं।
- अक्सर इन्हें गुप्त और रहस्यमयी समझा जाता था।
🔷 खंड II: कर्नाटक में वीरशैव परंपरा
● लिंगायत या वीरशैव आंदोलन
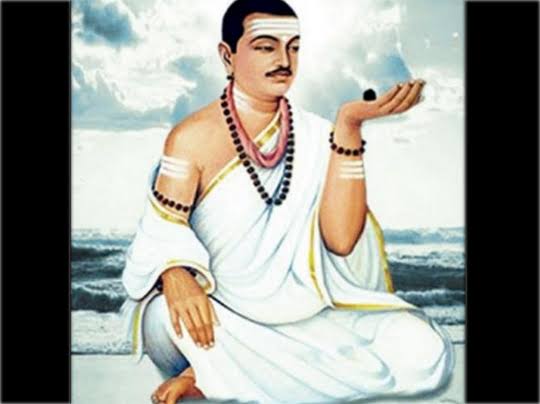
- 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना द्वारा शुरू किया गया आंदोलन।
- उन्होंने जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व, और वेदों को खारिज किया।
- शिव को लिंग रूप में पूजा जाता था।
- सरल एकेश्वरवाद, आंतरिक पवित्रता, और मंदिर पूजा का विरोध इनकी विशेषताएँ थीं।
- विधवा विवाह, स्त्री समानता, और कन्या शिक्षा का समर्थन किया।
- इनकी रचनाएँ वचन (Vachanas) कहलाती हैं, जो कन्नड़ भाषा में थीं।
🔷 खंड III: महाराष्ट्र के संत
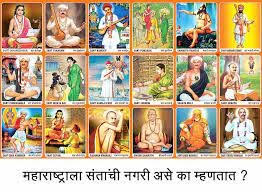
- प्रमुख संत: नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जनाबाई, सखुबाई।
- मुख्य बिंदु:
- विठोबा (विट्ठल) के प्रति भक्ति (विष्णु का रूप)
- जाति व्यवस्था का विरोध, समानता का प्रचार
- मंदिरवाद और कर्मकांड का विरोध
- इनकी रचनाएँ अभंग (Abhang) कहलाती हैं और ये मराठी में थीं।
🔷 खंड IV: नाथपंथी, सिद्ध और योगी
- इन्होंने कर्मकांड और पुजारियों के वर्चस्व का विरोध किया।
- सन्यास, ध्यान, और योगिक साधना को प्राथमिकता दी।
- शरीर को आध्यात्मिक अनुभव का माध्यम माना।
- इनकी रचनाएँ स्थानीय भाषाओं में थीं और आम लोगों तक पहुँचीं।
🔷 खंड V: उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन
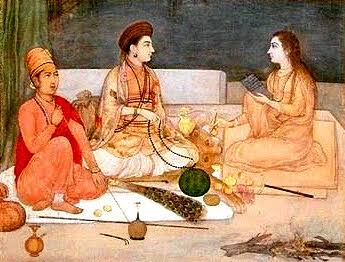
● मुख्य विशेषताएँ
- एक निराकार ईश्वर में विश्वास
- जाति भेद का विरोध
- बाह्य आडंबर, मंदिर, वेद और मूर्ति पूजा का विरोध
- प्रेम, भक्ति, और समर्पण पर बल
● कबीर (15वीं शताब्दी)
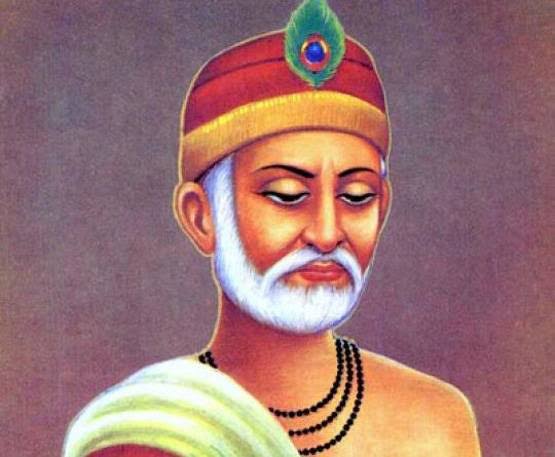
- निर्गुण ईश्वर में विश्वास
- उनकी भाषा साधारण हिंदी/अवधी/खड़ी बोली थी
- रचनाएँ: साखी और पद
- हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं की आलोचना
- मूर्ति पूजा, तीर्थ, और रोज़े का विरोध
- रचनाएँ: गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली में शामिल
● गुरु नानक (1469–1539)
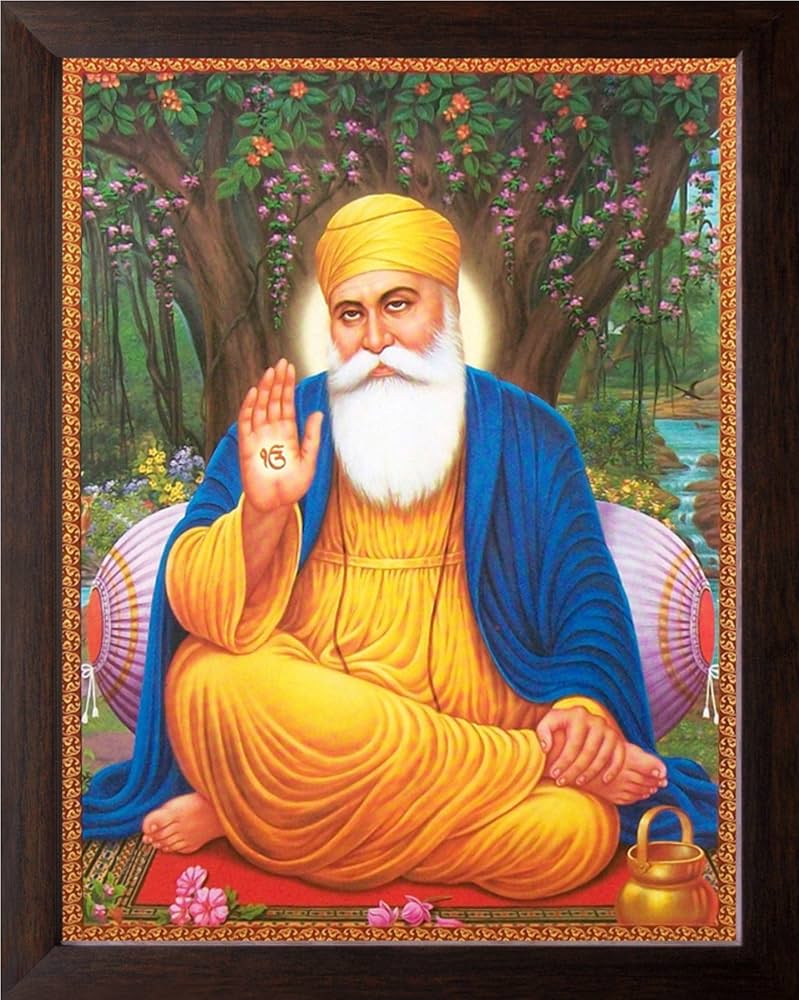
- सिख धर्म के संस्थापक
- पंजाबी में शिक्षाएँ दीं
- संगत (समूह) और लंगर (सामूहिक भोजन) की परंपरा शुरू की
- जाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध
- शिक्षाओं का संकलन: गुरु ग्रंथ साहिब
🔷 खंड VI: धार्मिक समुदायों के बीच संबंध
● परस्पर संवाद और संपर्क
- धर्मों में बातचीत, साझी परंपराएँ और कभी-कभी टकराव भी।
- साझे तीर्थ, त्योहार, भजन और कविताएँ आम रहीं।
- उदाहरण: अकबर का सुलह-ए-कुल, जहाँगीर की संतों के प्रति श्रद्धा।
🔷 खंड VII: सूफ़ी परंपराओं का विकास

● सूफ़ीवाद क्या है?
- इस्लामी रहस्यवाद जिसमें आंतरिक शुद्धता, ईश्वर के प्रति प्रेम, त्याग, और समता प्रमुख हैं।
- भारत में 8वीं शताब्दी से सूफ़ी मत का प्रसार हुआ।
● प्रमुख सूफ़ी सिलसिले (संप्रदाय)
- चिश्ती, कादिरी, सुहरावर्दी, नक्शबंदी
- इनकी शिक्षाएँ गुरु-शिष्य परंपरा में चलती थीं
● चिश्ती सिलसिला
- भारत में इसकी शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती (अजमेर) ने की।
- अन्य संत: निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, नसीरुद्दीन चिराग़ देहलवी
- परंपराएँ:
- समा (धार्मिक संगीत)
- लंगर (भंडारा)
- समानता और करुणा
- सभी धर्मों के लोगों का स्वागत
● सूफ़ी खानकाह
- सूफ़ी संतों के निवास स्थल जहाँ शिष्य भी रहते थे
- चर्चा, साधना, सेवा, और भंडारे का केंद्र
● सूफ़ी साहित्य
- मलफ़ूज़ात (वाणी), मकतूबात (पत्र), तज़किरा (जीवनियाँ)
- फारसी और स्थानीय भाषाओं में कविताएँ और भजन
- संतों की दरगाहें आस्था के केंद्र बन गईं
🔷 खंड VIII: नई भक्ति धाराएँ और मंदिर परंपराएँ
● मंदिर और धार्मिक संस्थाएँ
- भक्ति और सूफ़ी आंदोलन के विरोध के बावजूद मंदिरों का महत्व बना रहा
- राजा मंदिरों का संरक्षण करते थे
- मंदिर केवल पूजा के नहीं बल्कि:
- सामाजिक आयोजन,
- शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों,
- संगीत और नृत्य,
- अर्थव्यवस्था के भी केंद्र थे
● स्त्रियाँ और भक्ति आंदोलन
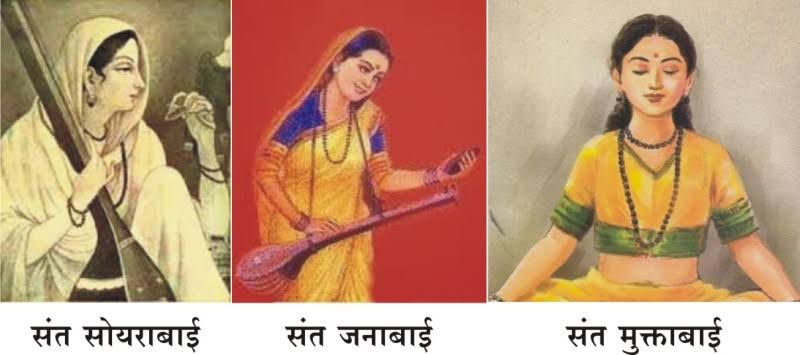
- मीराबाई, अंडाल, लल्लेश्वरी, जनाबाई जैसी स्त्रियाँ इस आंदोलन की प्रमुख थीं।
- मीराबाई (16वीं शताब्दी):
- कृष्ण भक्ति की प्रतीक
- राजपरिवार की परंपराओं को ठुकराया
- राजस्थानी और ब्रज भाषा में भजन लिखे
- प्रेम और समर्पण की प्रतीक
🔷 निष्कर्ष
- भक्ति और सूफ़ी आंदोलनों ने धार्मिक संकीर्णताओं को चुनौती दी।
- इनका ज़ोर था:
- प्रेम,
- समानता,
- आध्यात्मिक स्वतंत्रता,
- जातिवाद और कर्मकांड का विरोध
- इनकी साझा विरासत आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करती है।
✅ अध्ययन फल (Learning Outcomes)
- छात्र मध्यकालीन भारत की धार्मिक परंपराओं को समझ पाते हैं।
- भक्ति और सूफ़ी परंपराओं की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं।
- इन आंदोलनों के सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हैं।