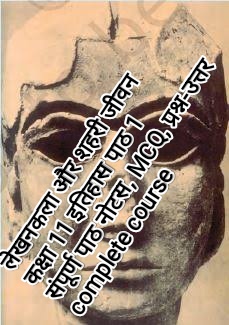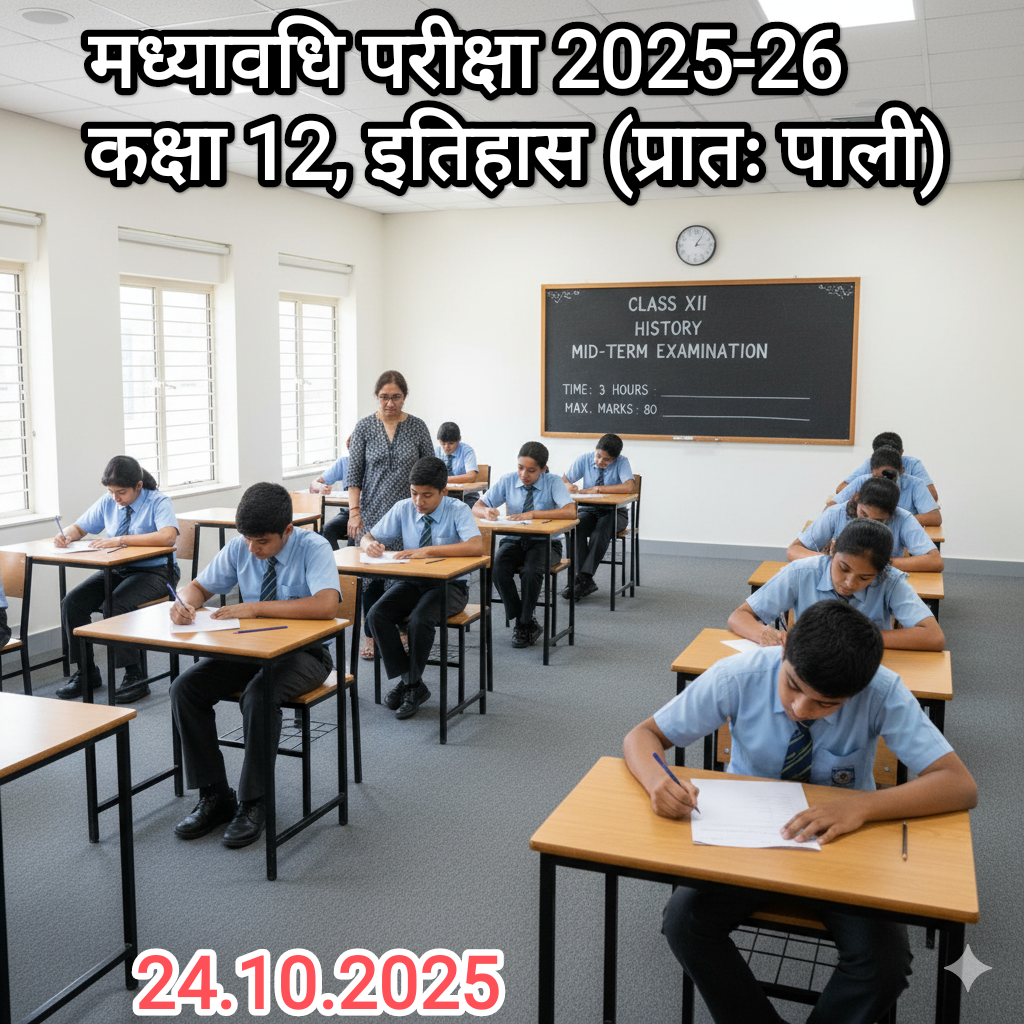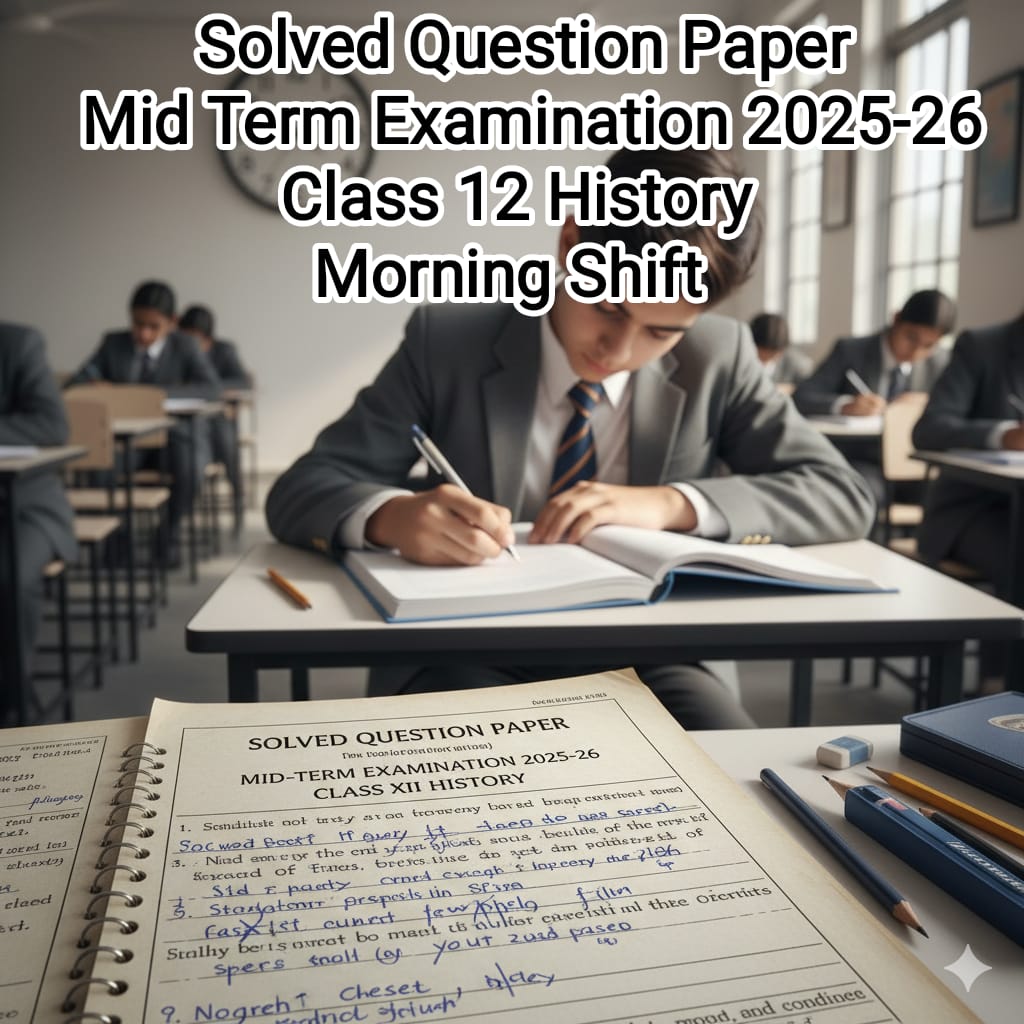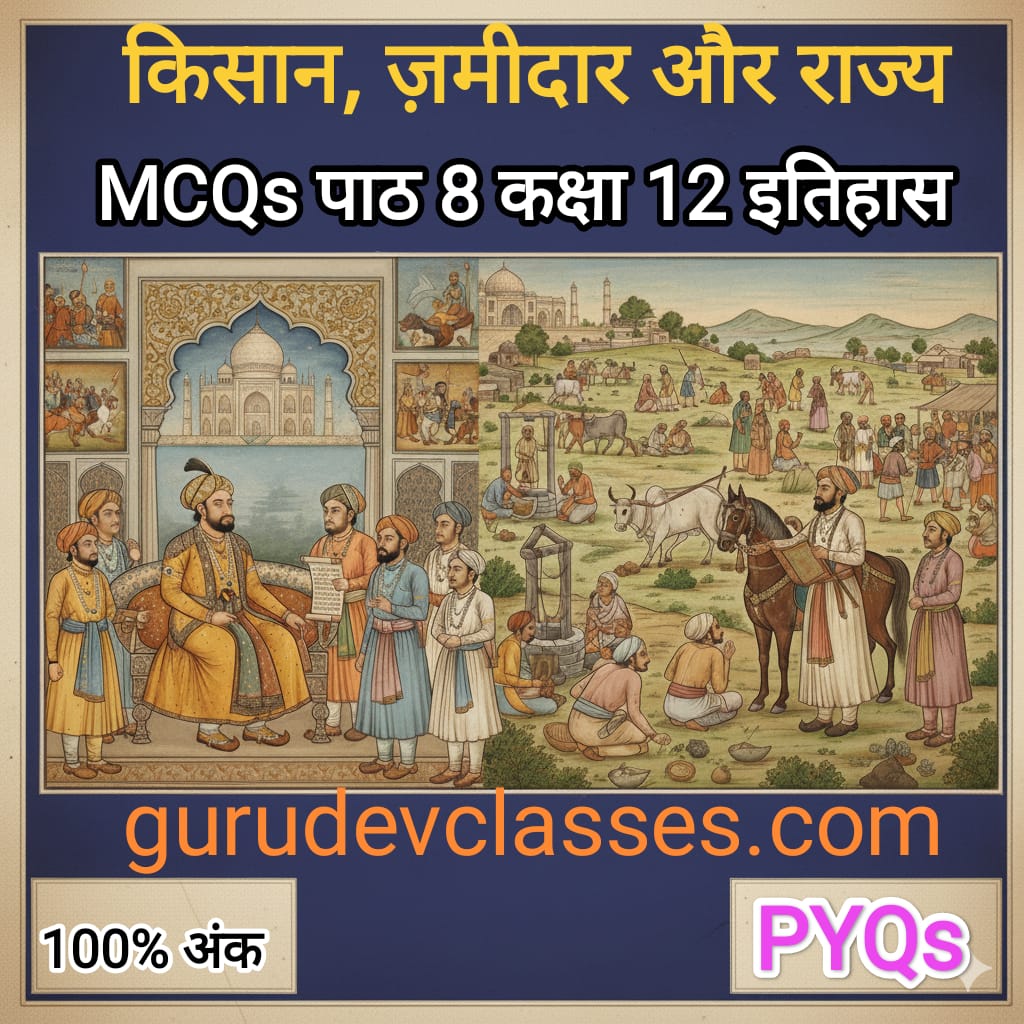परिचय
कांसे के प्रयोग से मानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और मानव जीवन का सामाजिक संबंध अधिक विस्तृत हो गया। जहां कांसे के औजार और हथियार प्रयोग में आने लगे, वहां आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रगति होने लगी। व्यापार में विकास होने के कारण आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति हुई। फलतः संपत्ति का प्रश्न जटिल हो गया और उसकी रक्षा के लिए नियम, कानून आदि की आवश्यकता पड़ी। फिर, नगरों के जीवन के जटिल होने के कारण सार्वजनिक जीवन के नियमन के लिए एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। फलतः कालांतर में समाज में शासकों और राजाओं का उदय हुआ, जिसे आज हम सरकार कहते हैं। धीरे-धीरे जनसमूहों ने विभिन्न व्यवसाय अपनाए। कुछ लोगों ने विशेष शिल्पों में दक्षता प्राप्त की। फलतः श्रम विभाजन का आरम्भ हुआ। मनुष्य के अनुभव संचित करने के लिए लेखनकला का आविष्कार हुआ। इसी तरह, लेन-देन की सुविधा के लिए मुद्रा का भी आविष्कार किया गया। इस तरह लगभग 4000 वर्ष पूर्व एक अन्य क्रांति हुई, जिसे ‘शहरी क्रांति’ कहते हैं। इसका प्रतिनिधित्व करने वाली सभ्यता का नाम था ‘मेसोपोटामिया सभ्यता’ ।
इराक को प्राचीनकाल में ‘मेसोपोटामिया’ के नाम से जाना जाता था। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों ‘मैसो’ तथा ‘पोटम’ से मिलकर बना है। ‘मैसो’ का अर्थ मध्य तथा ‘पोटम’ का अर्थ नदी होता है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है। प्राचीन इराक क्षेत्र में बहने वाली दो नदियां ‘दजला’ और ‘फरात’ थीं। इस प्रकार ‘दजला’ और ‘फरात’ नदियों के मध्य स्थित प्रदेश को मेसोपोटामिया कहा जाता था। ये नदियां हर साल काफी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी इस प्रदेश में जमा करती थीं, जिसके कारण यह क्षेत्र काफी उपजाऊ था। इन नदियों में बहुत-सी नहरें भी बनाई गई थीं, जिनसे इस क्षेत्र के दूर-दूर के भागों तक सिंचाई होती थी। इन नदियों को यातायात के लिए भी प्रयोग किया जाता था, जिनमें नावें चला करती थीं। इनके किनारे-किनारे कारवां भी चलते थे। इस प्रकार यह क्षेत्र एक सबल सभ्यता के विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त था। मेसोपोटामिया क्षेत्र केवल दजला व फरात नदियों के मध्य तक सीमित न होकर फारस की खाड़ी के दक्षिण तक विस्तृत था। इस क्षेत्र को तीन प्रदेशों में बांटा जा सकता है-प्रथम दजला फरात के बीच का क्षेत्र (दोआब) जिसको असीरिया कहा जाता है, दूसरा संगम से सटा क्षेत्र अक्कद तथा तीसरा-सुमेर । इन्हीं तीन क्षेत्रों में प्राचीन काल में चार सभ्यताएं विकसित हुईं, जिन्हें असीरियन एवं कैल्डीयन, बेबीलोनियन एवं सुमेरियन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता के अन्तर्गत उपरोक्त चारों सभ्यताएँ आती हैं। इन सभ्यताओं के बारे में कहा जाता है कि सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोन ने उसे चरम सीमा तक पहुँचाया तथा असीरिया ने उसे ग्रहण किया। इन सभ्यताओं में सबसे पहले ‘सुमेरिया’ की सभ्यता का विकास हुआ। इस अध्याय के अन्तर्गत हम मेसोपोटामिया सभ्यता के काल की भाषा, लेखन तथा शहरी जीवन के विविध पहुलओं को समझने का प्रयास करेंगे।
पारिभाषिक शब्द
मेसोपोटामिया यह नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेमोस तथा पोटैमोस से मिलकर बना है। मेमोस का अर्थ ‘मध्य’ तथा पोटैमोस का अर्थ ‘नदी’ होता है। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ बना नदी के बीच का क्षेत्र। यह शब्द दजला-फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है।
नोआ-बाईबल में वर्णित यह व्यक्ति जिसे ईश्वर ने जलप्लावन से जीवन बचाने के लिए चुना था। बाईबल के अनुसार, इसी व्यक्ति ने सभी जीव-जंतुओं का एक-एक जोड़ा अपनी नाव में रखकर उन्हें जलप्लावन से सुरक्षित बचाया था।
जिउसूद्र-मेसोपोटामिया साहित्य का वह नायक जिसने जलप्लावन की घटना से जीवों को बचाया था। बाईबल के नोआ नायक की तरह इसे जलप्लावन की घटना के समय का नायक बताया गया है। मेसोपोटामिया साहित्य में इसे ‘उतनापिष्टिम’ भी कहा गया है।
काँसा धातु-इस धातु का निर्माण ताँबे और राँगे (टिन) के मिश्रण से होता है। मेसोपोटामिया सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता का दर्जा प्राप्त है अर्थात् इस युग की मुख्य धातु ‘काँसा’ थी।
क्यूनीफार्म अथवा कीलाकार-यह लातिनी भाषा का शब्द है। क्यूनीयस का अर्थ ‘खूँटी’ और फोर्मा का अर्थ ‘आकार’ होता है। मेसोपोटामिया की लिपि कीलाकार ही थी।
स्टेल-यह पत्थर के ऐसे शिलापट्ट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते हैं।
एकल परिवार-इस तरह के परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चे शामिल होते हैं।
हौज-जमीन में एक ऐसा ढका हुआ गड्ढा, जिसमें पानी और मल जाता है।
शडूफ-सिंचाई की एक तकनीक, जिसे ‘रहट’ सिंचाई प्रणाली के समकक्ष माना जा सकता है।
सुमेर-मेसोपोटामिया के दक्षिण क्षेत्र को इस नाम से जाना जाता था। इसी क्षेत्र में पहले-पहल नगर उदित हुए।
हम्मुराबी विधि संहिता-इसे पत्थर की शिला पर खोदा गया था, ताकि सब लोग कानूनों को जान सकें। इसे सबसे प्राचीन विधि संहिता माना जाता है। इसे राजा हम्मुराबी ने बनवाया था।
जिगुरात मंदिर का वह ऊंचा स्थल जिस पर पक्की ईंटों से देवस्थल बना होता था, उसे जिगुरात कहा जाता था। जिगुरात का शाब्दिक अर्थ ‘स्वर्ग की पहाड़ी’ है।
शहर-इसे अंग्रेजी भाषा में सिटी (City) कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के शब्द ‘सिवीतास’ से बना है। इस शब्द का प्रयोग शुरू में यूनान के विकसित नगर राज्यों के लिए होता था।
पेपिरस मिस्र में लगभग 3000 ई. पू. में पेपिरस नामक पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखा जाता था। अंग्रेजी भाषा का शब्द ‘पेपर’ इसी पेपिरस से बना है।
पेट्सी-मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर-राज्यों के पुरोहितों को इस नाम से जाना जाता है।
प्रश्न 1. मेसोपोटामिया के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए।
उत्तर- मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। आर्थिक संसाधनों पर ज्यादातर इसी छोटे से वर्ग का नियन्त्रण था। उर नगर में राजाओं और रानियों की कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई वस्तुएँ (आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियाँ, लाजवर्द से अलंकृत लकड़ी के वाद्य, सोने के सजावटी खंजर) इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोगों के जीवनयापन के साधनों में भारी अंतर था। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन के विविध पहलुओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
A) परिवार (Family)- विवाह, उत्तराधिकार आदि से संबंधित कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के शहरी समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। एकल परिवार से हमारा अभिप्राय ऐसे परिवार से है, जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी व बच्चे शामिल होते हैं। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार आमतौर पर अपने माता-पिता के साथ ही रहा करता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता की सम्पत्ति पर उसके पुत्रों का ही अधिकार होता था।
B) विवाह (Marriage) – इस समाज में विवाह प्रायः माता-पिता की सलाह से ही किया जाता था। वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद दोनों परिवारों (वर व वधू) आपस में उपहारों का आदान-प्रदान करते थे तथा उनके बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता था। इसके बाद दोनों परिवार मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थेl
C) निवास स्थान (Residence)- शहरों में मकान प्रायः ईटों से बने होते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में पत्थर का अभाव था। ईंटें धूप में सुखाकर तैयार की जाती थीं। घरों को सजाने के लिए कालीन, पर्दो, फूलदान, हाथी दांत से बनी मूर्तियाँ व सोने के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। घर का मुख्य दरवाजा किसी दूसरे के घर की ओर नहीं खुलता था। शायद ऐसा घर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए किया जाता हो। ऊँची दहलीज वाले घरों को शुभ माना जाता था।
D) नगर-नियोजन (Town Planning)- मेसोपोटामिया के शहर नियोजित नहीं थे। इन शहरों की गलियाँ तंग, पतली, टेढ़ी-मेढ़ी व घुमावदार होती थीं। इन गलियों की दुर्दशा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी भारी सामान गधों की सहायता से ही मकानों में पहुँचाया जा सकता था। घरों से जल-निकासी की व्यवया भी अच्छी नहीं थी। वर्षा के दिनों में गली का पानी घरों में घुस जाता था। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं, अपितु उन दरवाजों से आती थी जो आँगन में खुलते थे। इस तरह कह सकते हैं कि इन शहरों का नगर-नियोजन साधारण दर्जे का भी नहीं था।
E) पहनावा (Dress)- संपन्न वर्ग के लोग सोने के आभूषण तथा कीमती पत्थरों की माला पहनते थे। उच्चवर्ग के लोग अपने शरीर के वस्त्रों पर इत्र (सुगंधित पदार्थ) का प्रयोग करते थे। वे हाथ में छड़ी रखते थे, जिसका ऊपरी सिरा मुहरों से अलंकृत होता था। समान्य पुरुष लुंगी अथवा तहमद का प्रयोग करते थे। इनका ऊपर का शरीर नंगा रहता था। घर में काम करने वाले सेवक व सेविकाएँ कमर में नीचे का तन ढकने के लिए बहुत साधारण वस्त्रों का प्रयोग करते थे। गरीब लोग सामान्यतः पाँवों में चप्पल जैसी कोई वस्तु नहीं पहनते थे।
F) धार्मिक विश्वास (Religious Believes)- मिस्र के लोगों की तरह मेसोपोटामिया के लोगों का परलोक के जीवन में कतई विश्वास नहीं था। इस समाज का पुरोहित वर्ग भी धार्मिक कार्यों के साथ व्यावसायिक कार्यों में अपनी हिस्सेदारी रखता था। सही मायनों में उनका धर्म परलौकी न होकर व्यावहारिक ज्यादा था। तन्त्र-मन्त्र में ये लोग विश्वास करते थे। इसलिए बुरी आत्माओं, रोग, मृत्यु व अकाल से बचने के लिए वे देवी-देवताओं की पूजा, जादू-टोना, ताबीज व मन्त्रों का जाप करते थे।
G) शिक्षा (Education) – मेसोपोटामिया के शहरी समाज में छात्रों को ज्योतिष, गणित, धर्म, शारीरिक व्यायाम व चिकित्सा शास्त्र आदि विषय पढ़ाए जाते थे। इस कार्य के लिए मंदिरों के पास ही विद्यालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए थे। शहरों में साक्षरता का स्तर नीचा था, परन्तु फिर भी समाज में शिक्षा का महत्त्व कायम था।
H) शवाधान (Burial) उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जन-साधारणकी समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए प्राप्त हुए हैं। इससे आभास होता है कि इस शहरी समाज में शवों को दफनाने का रिवाज ज्यादा प्रचलित था।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया का शहरी जीवन उच्च वर्ग व पुरोहित वर्ग की छत्रछाया में पल रहा था। शहरों में नगर-नियोजन का सर्वथा अभाव था।
प्रश्न 2. मानय इतिहास पर लेखन कला का क्या प्रभाव पड़ा?
उत्तर- मानव को सभ्य और विकसित बनाने में लेखन कला का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसलिए लेखन कला के आविष्कार को मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। इस कला के फलस्वरूप ही समझौतों, आदेशों व कानूनों को दस्तावेजों का रूप देना संभव हो पाया। सही अर्थों में इस कला ने ही मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। मानव इतिहास को तार्किक, स्पष्ट व सरल बनाने में भी इसके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मानव इतिहास पर लेखन कला के प्रभाव को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
a) सांस्कृतिक प्रभाव (Cultural Impacts)-
लेखन ने मानव के सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक चेतना को सकारात्मक रूप से काफी प्रभावित किया। सुमेरियन व अवकदी भाषाओं के विकास में इस कला का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। लेखन कला की बदौलत ही साहित्य की रचना हुई। मेसोपोटामिया का उपलब्ध सबसे प्राचीन महाकाव्य (लंबी कविता) गिल्गेमिश इसका सुन्दर उदाहरण है। लेखन कला के विकास में मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का विशेष योगदान रहा है। दुनिया की सभी भाषाओं का विकास लेखन कला की बदौलत ही हुआ।
b) आर्थिक प्रभाव (Economic Impacts)-
कहानियों और किस्सों जैसी परम्परा को तो मौखिक रूप से एक-दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, परन्तु विज्ञान और आर्थिक विषयों के संबंध में ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए लेखन कला की अत्यन्त आवश्यकता होती है। लेखन कला ने ही वाणिज्य व व्यापार को नया शिखर प्रदान किया। इसके फलस्वरूप व्यापारिक समझौतों को लिखित रूप दिया जाने लगा, जिससे इनकी साख बढ़ी। व्यापार में प्रयुक्त होने वाली मोहरों पर लेख-लिखे जाने से व्यापार में पारदर्शिता आई। विदेशी व्यापार को विकसित करने में भी लेखन कला महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता के बीच होने वाला व्यापार इसी तरह की लिखित मोहरों पर आधारित था। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिना लेखन कला के आर्थिक विकास कतई सम्भव नहीं था।
C) सामाजिक प्रभाव (Social Impact) :-
सामाजिक जीवन पर लेखन कला के प्रभाव को मेसोपोटामिया की इस कहावत से समझा जा सकता है कि, “जो पट्टिकाएँ लिखने में प्रवीण होगा, वह सूर्य की तरह चमकेगा।” इस कहावत से समझा जा सकता है कि प्राचीन समाज में लेखन कला जानने वाला कितना महत्त्वपूर्ण रहा होगा। इससे उस समय के समाज में एक ऐसे लिपिक वर्ग का उदय हुआ, जिसका महत्त्व पुरोहितों के समान था। सामाजिक चिंतन व सामाजिक संरचना को विकसित करने में इस कला का सबसे ज्यादा योगदान रहा। इसने शासकों के लिखित आदेशों के माध्यम से सामाजिक जीवन को संगठित किया। अधिकार व कर्तव्य जैसे विषयों को सामान्य जन तक पहुँचाने का कार्य भी इसके माध्यम से हुआ। कानूनों को सर्वव्यापी बनाने में इसका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बेबीलोनिया के राजा हम्मुराबी की विधि-संहिता इसका सबसे सुन्दर उदाहरण है। सामाजिक रीति-रिवाजों, परम्पराओं व विरासत को संजोकर रखने में इसके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
d) राजनीतिक प्रभाव (Political Impact) –
लेखन कला के माध्यम से ही शासक अपनी प्रजा पर राजनीतिक व प्रशासनिक नियन्त्रण स्थापित करने में सफल रहे। शासकों ने अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदवाया तथा उन्हें दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थापित करके अपने आदेशों को आम जनता तक पहुँचाया। इस तरह के प्रशासकीय नियन्त्रण के फलस्वरूप ही आगे चलकर विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। शासकों की वंशावली व शासनकाल अवधि को प्रामाणित करने में लेखनकला का विशेष योगदान रहा। इस कला के माध्यम से ही राजनैतिक उत्तराधिकार के नियम, सत्ता हस्तांतरण के नियम व कानून सार्वजनिक हो पाए। पाषाणशिलाओं पर लिखे राजनीतिक लेख आज हमारे राजनैतिक अध्ययन के मुख्य आधार स्तम्भ स्रोत हैं।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं था, जिसे लेखन कला ने सकारात्मक रूप से प्रभावित न किया हो। धार्मिक अनुष्ठानों, राजनैतिक वंशावलियों, सामाजिक रीति-रिवाज व परम्पराओं, साहित्य व भाषा तथा व्यापार व वाणिज्य के सभी तत्कालीन पहलुओं का ज्ञान करवाने में लेखन कला हमारी सबसे ज्यादा सहायता करती है। सर्वप्रथम लेखन की शुरूआत मेसोपोटामिया से हुई, इसलिए सम्पूर्ण मानव समाज सदैव इसके लिए मेसोपोटामिया सभ्यता का ऋणी रहेगा।
प्रश्न 3. मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों के प्रकार का उल्लेख कीजिए।
उत्तर- लगभग 5000 ई. पू. के आसपास मेसोपोटामिया में शहरीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ हो गया था। इस शुरूआती दौर में सबसे पहले दक्षिणी मेसोपोटामिया में वस्तियों का विकास हुआ। इन बस्तियों में से धीरे-धीरे कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई प्रकार के थे अर्थात् सभी एक जैसे नहीं थे। उदय व विकास की दृष्टि से इनकी अलग-अलग विशेषताएँ थीं, जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
A) मंदिर केन्द्रित शहर (Temple Based City) –
दक्षिणी मेसोपोटामिया में बाहर से आने वाले लोगों ने अपने निवास क्षेत्र के आस-पास मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। शुरू के मंदिर एक छोटे से देवालय के समान थे, जिसको बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। धीरे-धीरे ये मंदिर विभिन्न देवी-देवताओं के निवास स्थान बनने लगे। उर (चंद्रदेवता) और इन्नान (प्रेम व युद्ध की देवी) इसी तरह के उदाहरण हैं। समय के साथ बड़े होते इन मंदिरों के खुले आँगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। इसमें से कुछ शुरूआती मंदिर तो बिल्कुल साधारण घरों जैसे होते थे। इस तरह के मंदिरों को देवी-देवताओं का निवास-स्थल माना जाता था। साधारण घरों और इन मंदिरों में यही अन्तर था कि इन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ विशेष अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थीं। आराध्य देव सैद्धातिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। इसलिए स्थानीय लोग देवी-देवताओं के लिए उपहारस्वरूप अन्न, दही व मछली लाते थे। धीरे-धीरे ये मंदिर आस्था के केन्द्र बनने लगे तथा दूर-दराज से लोग आकर इन मंदिरों के समीप बसने लगे। इसके फलस्वरूप इन स्थानों पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ने लगीं। स्थानीय समुदायों के मुखियाओं और पुरोहितों ने उत्पाद मचाने वालों को नियंत्रित करके लोगों को सुरक्षा प्रदान की। धीरे-धीरे इन लोगों (मुखिया व पुरोहित) ने स्थानीय आर्थिक गतिविधियों पर भी अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया। आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि होने से इन मंदिरों ने मुख्य शहरी संस्था का रूप धारण कर लिया। मुखियाओं तथा पुरोहितों ने अपने आपको राजा (पेट्सी) के रूप में स्थापित कर लिया। देवताओं को कीमती भेंटें अर्पित करके, मंदिरों की धन-सम्पदा का वितरण करके, उत्पाती लोगों को हरा करके इन पेट्सी राजाओं ने स्थानीय जनता पर अपना प्रभुत्त्व स्थापित कर लिया। मंदिरों व स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए इन्होंने सेना रखनी भी शुरू कर दी। इस तरह मंदिर केन्द्रित शहरों का उदय व विकास हुआ।
B) व्यापार केन्द्रित शहर (Trading Based City)
शहरों के उदय व विकास में व्यापारिक गतिविधियों की भूमिका सदा से ही निर्णायक रही है। इसलिए मेसोपोटामिया में भी कुछ ऐसे शहरों का उदय हुआ, जिनकी नींव विशुद्ध रूप से व्यापार पर टिकी थी। आगे चलकर मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों का केन्द्र-बिन्दु होने के कारण मेसोपोटामिया के कुछ शहर व्यापार केंद्रित शहरों के रूप में उभरे। इस तरह के शहर मुख्यतः व्यापारिक मार्गों और नदियों के किनारे फले-फूले। मेसोपोटामिया का ‘मारी’ शहर इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह भौगोलिक दृष्टि से फरात नदी के किनारे स्टेपी (घास के मैदानी क्षेत्र) क्षेत्र में पड़ता था। इस क्षेत्र से होने वाले व्यापारिक जल-मार्ग का यह केन्द्र-बिन्दु बनकर उभरा, क्योंकि इसी मार्ग से दक्षिण में सुमेर, उत्तर में तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच व्यापार होता था। एमोराइट, असीरियाई, आर्मीनियन व अक्कदी जैसे पशुपालक समुदाय इस क्षेत्र में रहते थे, जो अक्सर व्यापारियों का माल लूट लेते थे। व्यापार को सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक ढाँचा तैयार किया गया। इसी प्रशासनिक ढाँचे पर आगे चलकर यह शहर एमोराइट समुदाय के शासकों की राजधानी के रूप में खूब फला-फूला। इस शहर की भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ‘जिमलिम’ नामक शासक लगभग 260 कमरों वाले 2.4 हेक्टेयर में फैले एक भव्य महल में रहता था। ‘मारी’ शहर विशुद्ध रूप से एक व्यापार केंद्रित शहर था, क्योंकि इसके आस-पास की जमीन भी अधिक उपजाऊ न थी।
C) सत्ता केंद्रित शहर (Imperial Based Cities)
मेसोपोटामिया में शहरीकरण की जो प्रक्रिया मंदिर केंद्रित व व्यापार केंद्रित शहरों से शुरू हुई थी, वह सत्ता केन्द्रित शहरों पर जाकर पूर्ण हुई। इन सत्ता केन्द्रित शहरों को सामान्य भाषा में शाही शहरों की संज्ञा भी दी जा सकती है। ये ऐसे शहर थे, जिनके उदय और विकास में ‘सत्ता’ की हिस्सेदारी काफी महत्त्वपूर्ण रही। इस तरह के शहर आरम्भ में स्थानीय शासकों के नियन्त्रण में रहे और बाद में इनमें से कुछ बड़े-बड़े नगर राज्यों की राजधानी के रूप में विकसित हुए। इन राजधानी शहरों के शासक भव्य महलों में रहते थे तथा भोग-विलास से पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इन शासकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने व अपने लिए अच्छे अवसरों की तलाश में दूर-दूर से दस्तकार, कारीगर, व सेवादार यहाँ आकर बसने लगे। शासक, दरबारी, व्यापारी, सैनिक अधिकारी, पुरोहित, सैनिक आदि का एक ऐसा विशाल समूह इन शहरों में स्थापित हो चुका था, जो पूरी तरह से किसी न किसी रूप में सत्ता की हिस्सेदारी से जुड़ा हुआ था। ये शहर आकार तथा भव्यता की दृष्टि से काफी विशाल थे।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया में अलग-अलग परिस्थितियों व अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार के शहरों का उदय व विकास हुआ। मंदिर केंद्रित, व्यापार केंद्रित व सत्ता केंद्रित शहरों ने मिलकर दुनिया की प्रथम शहरीकरण की प्रक्रिया को उसकी मंजिल तक पहुँचाया।
प्रश्न 4. मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए।
उत्तर: आधुनिक इराक और प्राचीन मेसोपोटामिया भौगोलिक दृष्टि से विविधता वाला देश है। इस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 7000 से 6000 ई. पू. के बीच कृषि की शुरूआत हो गई थी। हरे-भरे, ऊँचे-नीचे मैदान, वृक्षाच्छादित पर्वत-श्रृंखला, स्वच्छ झरनों तथा पर्याप्त वर्षा ने शायद इसमें मदद की हो। प्राचीन समय में कृषि की अपेक्षा पशुपालन आजीविका का अच्छा साधन था। इस दृष्टि से भी मेसोपोटामिया की भूमि काफी अनुकूल थी, क्योंकि यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं तथा पशुओं के चरने के लिए चारे की कोई कमी नहीं है। भेड़-बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी-छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण-पोषण आसानी से कर सकती थीं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ जल-परिवहन का अच्छा साधन हैं। इसका दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। यह वही स्थान है जहाँ दुनिया के प्रथम शहर बने तथा लेखन कला का विकास हुआ। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का व्यवस्थित अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है-
a) दक्षिणी भाग (Southern Part) –
भौगोलिक दृष्टि से मेसोपोटामिया का यह भाग सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसी भाग में पहली बार शहर का निर्माण व लेखन कला का विकास हुआ इस भाग में आजीविका के भरपूर साधन उपलब्ध थे। इस भाग को उपजाऊ बनाने में दजला व फरात नदियों का विशेष योगदान रहा, क्योंकि ये नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। वर्षा के समय इन नदियों में बाढ़ के रूप में जो पानी एकत्रित होता है, उसे सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है। इससे वहाँ उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए सभी पुरानी सभ्यताओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। यह स्थिति तब थी, जब वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी।
b) पूर्वोत्तर भाग (Eastern Part)-
मेसोपोटामिया का पूर्वोत्तर भाग हरे-भरे पेड़ों, ऊँचे-नीचे मैदानों तथा वृक्षाच्छादित पर्वत-श्रृंखलाओं से परिपूर्ण है। इसकी पर्वत श्रृंखलाओं पर ऊँचे-ऊँचे पेड़ों का अपार फैलाव है, जिसके कारण यहाँ की पर्वत-श्रृंखलाएँ ऊपर से ढकी हुई नजर आती हैं। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर स्वच्छ झरनों और जंगली फल-फूल व वनस्पति की कोई कमी नहीं है। यह क्षेत्र ऊँचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ बाढ़ जैसा कोई खतरा नहीं है। भेड़-बकरियाँ पालने के लिए प्राकृतिक रूप से यह पूर्णतः उपयुक्त स्थल है। अच्छी वर्षा होने के कारण यहाँ फसल भी अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल (पिंड खजूर) देते हैं।
C) उत्तरी भाग (Northern Part)-
मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग ऊँची भूमि के रूप में विस्तृत है, जिसे ‘स्टेपी’ (घास के मैदान) ने पूरी तरह से घेर रखा है। इस क्षेत्र में पशुपालन खेती की अपेक्षा आजीविका का ज्यादा बेहतर साधन है। यहाँ उगने वाली वनस्पति तथा घास से भेड़-बकरियाँ आसानी से अपना पेट भर सकती हैं। इन भेड़-बकरियों से भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएँ मिलती थीं। इसके अतिरिक्त यहाँ बहने वाली नदियों में मछलियाँ भी पर्याप्त मात्रा में मिलती थीं। सर्दियों की वर्षा के बाद यह सारा क्षेत्र हरा-भरा हो जाता था।
d) दजला व फरात नदियाँ (Tigris and Euphrates Rivers)-
जैसा कि हम जानते हैं कि दजला व फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को ही मेसोपोटामिया कहा गया है। वास्तव में ये दोनों नदियाँ यहाँ के लोगों की जीवन-रेखाएँ थीं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए जल-परिवहन का मार्ग उपलब्ध करवाती हैं। इस मार्ग ने मेसोपोटामिया के व्यापार को काफी समृद्ध बनाया। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद आगे कई धाराओं या शाखाओं में बंटकर बहने लगती है। बाढ़ जैसी स्थिति में ये धाराएँ नहरों का काम करती थीं, जिससे खेतों की सिंचाई की जाती थी। इस तरह की सिंचाई से आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर और मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वास्तव में मेसोपोटामिया का भौगोलिक क्षेत्र विविधताओं से भरा हुआ है। इस अलग-अलग क्षेत्र में घास के मैदान, ऊँचे पेड़, वनस्पति, पर्वत श्रृंखलाएँ, रोगिस्तान तथा नदियों का वहना इसे भौगोलिक दृष्टि से विविध बनाता है।
प्रश्न 5. लेखन पद्धति के विकास का उल्लेख करते हुए, मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन पद्धति पर प्रकाश डालिए।
उत्तर- मानव ने क्रमिक विकास के तहत भाषा अथवा बोली का विकास बहुत पहले कर लिया था। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे भाषा की दृष्टि से मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहा जाता है। लेखन या लिपि से हमारा अर्थ है संकेतों या चिह्नों के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली उच्चारित ध्वनियाँ। जब इन उच्चारित ध्वनियों को चिह्नों का रूप दिया जाने लगा तो, इसे लेखन पद्धति की शुरूआत मानी जाती है। आरम्भ में इसे भाषा का लिखित रूप मात्र स्वीकार किया गया। मेसोपोटामिया के विशेष संदर्भमें लेखन प्रद्धति के क्रमिक विकास को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
a) लेखन की शुरूआत (Origin of Writing) –
लेखन कला के बिल्कुल शुरूआती समय में आदिमानव अपने भावों को प्रकट करने के लिए चित्रकारी का सहारा लेता था। इस चित्रकारी को ही आरंभिक लेखन व भाषा का प्रारंभिक रूप स्वीकार किया जाता है। इस काल में मानव किसी वस्तु या जानवर का बोध करवाने के लिए उसका चित्र बनाता था। अधिकतर इतिहासकार व विद्वान उन गुफा-चित्रों व कलाकृतियों को ही भाषा व लेखन का प्रारंभिक रूप मानते हैं, जिन्हें आदि मानव ने बनाया था। व्यवस्थित चित्र लेखन की शुरूआत मेसोपोटामिया के दक्षिणी नगर-राज्य सुमेर से मानी जाती है। इसका प्रमाण मेसोपोटामिया से प्राप्त वो पट्टिकाएँ (Tablet) हैं, जो लगभग 3200 ई. पू. की हैं। इन पट्टिकाओं पर बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। ये पट्टिकाएं चिकनी मिट्टी से बनी थीं तथा इन्हें आग में पकाया जाता था। इन पट्टिकाओं पर जो चिह्न मिले हैं उनसे यह आभास होता है कि शायद ये वहाँ के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने-जाने वाली वस्तुएं रही होंगी। जब समाज को अपने लेन-देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, तब व्यवस्थित व स्पष्ट लेखन कार्य शुरू हुआ।
b) प्रारंभिक लेखन विधि (Technique of Earlier Writing)
शुरूआती लेखन पेड़ों के पत्तों व उनकी छाल तथा पशुओं की खाल आदि पर किया जाता था। 3000 ई. पू. में मिस्र में पेपिरस नामक पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की कलम से लिखे लेख इसके साक्ष्य हैं। आगे चलकर इसी ‘पेपिरस’ से ‘पेपर’ बना, जिसका अर्थ ‘कागज’ है। मेसोपोटामिया के दक्षिणी नगर-राज्य की लेखन-शैली उपरोक्त शैली से पूर्णतः अलग तथा प्रभावी थी। यहाँ के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। ये लोग चिकनी मिट्टी को गूँध कर एक ऐसे आकार की पट्टी तैयार कर लेते थे, जिसे लिपिक (लिखने वाला) आसानी से एक हाथ में पकड़ सके। इसके बाद लिपिक इसकी चिकनी ऊपरी सतह पर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से गीली पट्टी पर चिह्न अथवा अक्षरों को खोद देता था। इन्हें धूप से सुखाकर मजबूत रूप दिया जाता था। एक बार सूखने के बाद इस पट्टी पर कुछ नहीं लिखा जा सकता था। नए काम के लिए नई पट्टिका की आवश्यकता होती थी। इसलिए हमें मेसोपोटामिया के उत्खनन स्थलों से सैकड़ों पट्टिकाएँ मिली हैं।
c) कीलाकार लिपि (Cuneifarm) –
गीली अथवा नम पट्टियों पर दवाकर या खोदकर चिह्न छापने की यह कला आगे चलकर ‘कीलाकार’ लिपि के रूप में विकसित हुई। क्यूनीफार्म लैटिन भाषा के दो शब्दों ‘क्यूनियस’ और ‘फोर्मा’ से मिलकर बना है। ‘क्यूनियस’ का अर्थ खूँटी और ‘फोर्मा’ का अर्थ आकार होता है। इस लिपि की शुरूआत भी चित्रों व चिह्नों से ही हुई थी। पट्टिकाओं पर अंकित होने वाले चित्र या चिह्न प्रायः उन वस्तुओं का बोध कराते थे, जो साधारण लेन-देन में काम आती थीं। परन्तु इस प्रकार की लिपि से विचारों की पूर्णतः अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए 2600 ई. पू. के आसपास मेसोपोटामिया के दक्षिण नगर-राज्य सुमेर के लोगों ने विशेष वर्णों से युक्त ऐसी लिपि को विकसित किया, जिससे विचारों व भावों को आसानी से समझा जा सकता था। इस लिपि में लगभग 550 वर्ण थे और प्रत्येक लिपिक को कम से कम 300 वर्षों का ज्ञान होना अति आवश्यक था। यही कारण है कि इस तरह के लिपिक प्रायः पेशेवर होते थे। इसलिए मेसोपोटामिया में यह कहावत प्रचलित थी कि, “जो पट्टिकाएं लिखने में प्रवीण होगा, वह सूर्य की तरह चमकेगा।”
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि का लेखन पद्धति के विकास में विशेष महत्त्व है। यह लिपि पश्चिम एशिया की प्राचीनतम ज्ञात लिपि है।
प्रश्न 6. मेसोपोटामिया सभ्यता में शहरों के उदय व विकास में सहायक कारणों पर प्रकाश डालिए।
उत्तर:
a) भौगोलिक परिस्थितियाँ (Geographical Conditions) –
मेसोपोटामिया में गाँव से कस्बों और फिर कस्बों से शहरों का विकास कुछ विशेष परिस्थितियों में हुआ। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ थी तथा सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता ने इसे और भी ज्यादा उपयोगी बना दिया था। नदियों से निकलने वाले जल-मार्गों ने व्यापार को विशेष रूप से उन्नतशील बनाया। कृषि व पशुपालन के अनुकूल जलवायु व वनस्पति ने इसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में विशेष योगदान दिया। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध वन-संपदा ने भी शहरों के उदय व विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। स्टेपी घास के मैदानों ने पशुपालन को व्यवसाय का रूप प्रदान किया।
b)कृषि का विकास (Development of Agriculture) –
प्राचीनकाल में शहरों के उदय और विकास में कृषि की भूमिका निर्णायक रही। इस दृष्टि से मेसोपोटामिया के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात् सुमेर ने काफी उन्नति कर ली थी। इसलिए सबसे पहले इसी क्षेत्र में शहरों का उदय हुआ। शासक वर्ग कृषि के विकास में विशेष रुचि लेते थे। इसके फलस्वरूप खेती के लिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। हलों में बैलों को जोतने की शुरूआत हो चुकी थी। इन सबके फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिसे नजदीक के व्यापारिक स्थलों पर बेचा जाने लगा। इस तरह कृषि के विकास ने मेसोपोटामिया में शहरों के उदय के लिए आधारभूत ढाँचा तैयार किया।
c) तकनीकी विकास (Technology Development)-
शहरों के उदय व विकास में तकनीक का विशेष योगदान रहा है। मानव को औजारों का निर्माण करने में सक्षम होने के कारण ही अन्य जीवों से अलग माना गया है। एक प्राचीन कहावत है कि “औजार बदलने से इतिहास बदलता है।” यह कहावत मेसोपोटामिया के शहरों के उदय एवं विकास पर पूरी तरह से लागू होती है। यहाँ कृषि व गैर कृषि कार्यों दोनों में ही काफी तकनीकी परिवर्तन हुए। कृषि में हल जोतने के लिए वैलों का प्रयोग तथा चाक के बर्तन बनाने का प्रयोग कुछ इसी तरह के उदाहरण हैं। इस तरह के तकनीकी आविष्कारों ने व्यावसायिक व अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया में शहरों के उदय व विकास में तकनीकी विकास का काफी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
d) उद्योग (Industries) –
मेसोपोटामिया के लोग कांसा बनाना जानते थे और सोना, चाँदी व शीशे से भली भाँति परिचित थे। रथ बनाना इनका प्रमुख उद्योग-धंधा था, फर्नीचर आदि बनाने का कार्य भी यहाँ प्रचलित था। बढ़ई, लुहार और जुलाहे आदि सभी अपने कार्यों में अति निपुण थे। ये तांबे को पीटकर उससे विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ तथा अस्त्र-शस्त्र बनाते थे। धीरे-धीरे इन औद्योगिक कार्यों का उत्पादन बढ़ता गया। आगे चलकर इन लोगों ने अपने आपको विशेष क्षेत्रों में स्थापित कर लिया। इसलिए कहा जा सकता है कि कृषि व धातु पर आधारित प्रारंभिक छोटे उद्योगों ने भी प्रारंभिक शहरीकरण की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से अपना योगदान दिया।
e)व्यापार (Trade)-
सुमेर मेसोपोटामिया के व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। इसलिए मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहरों का उदय इसी क्षेत्र में हुआ था। यहाँ से अन्य देशों को कपड़ा, विलासिता का सामान और खजूर आदि का निर्यात होता था। दजला व फरात नदियों और उनकी धाराओं ने यहाँ के लोगों को सरल तथा सुगम जल-मार्ग उपलब्ध करवाया। विदेशी व्यापार मुख्यतः जलमार्गों से होता था। व्यापार अधिकतर मन्दिरों के पुरोहितों, व्यापारियों और सौदागरों के हाथ में था। पूर्व में इनके व्यापारिक केन्द्र सिन्धु घाटी व भूमध्य सागर के पूर्वी तट तक थे। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यापार की उन्नति ने भी शहरों के उदय व विकास में सहयोग किया।
f)व्यावसायिक दक्षता (Occupational Efficiency)-
हम पढ़ चुके हैं कि मेसोपोटामिया में कृषि में अधिशेष उत्पादन जैसी स्थिति आ चुकी थी। यहाँ कृषि उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। ऐसी स्थिति में बहुत-से लोग कृषि कार्य से मुक्त होने लगे। अब उनके पास अवसर था कि वे कोई भी स्वतन्त्र व्यवसाय अपना सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने अलग-अलग व्यवसाय अपनाए तथा उनमें दक्षता प्राप्त कर ली। इससे श्रम-विभाजन की अवधारणा को बल मिला तथा व्यवसाय का विशिष्टीकरण हुआ। आगे चलकर यही बात शहरों के उदय व विकास में सहायक बनी।
g)धर्म (Religion) –
मेसोपोटामिया में उभरने वाले आरंभिक शहर धर्म केंद्रित शहर थे। सुमेर के नगरों में स्थित मंदिर धार्मिक गतिविधियों के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के भी केन्द्र बनकर उभरे। इन मंदिरों के आस-पास विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोग आकर रहने लगे। मंदिरों के पुरोहितों ने इन्हें सुरक्षा प्रदान की। आगे चलकर यही पुरोहित पेटसी राजाओं के रूप में जाने गए। इस तरह हम कह सकते हैं कि धर्म और आस्था ने भी शहरों के उदय और विकास में अपना योगदान दिया।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी एक कारक की वजह से मेसोपोटामिया में शहरों का उदय व विकास नहीं हुआ, वरन इसके लिए उपरोक्त सभी कारण समान रूप से उत्तरदायी थे।
प्रश्न 7. मेसोपोटामिया के प्रारंभिक नगरों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
उत्तर- मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को काफी महत्त्व देते थे। इनमें अनेक समुदायों तथा संस्कृतियों के लोग साथ-साथ रहा करते थे। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग सुमेर में सबसे पहले नगरों का उदय हुआ था। उरुक, उर, बेबीलोन, निप्पूर, लगाश, मारी, निनेवे व अस्सुर मेसोपोटामिया के कुछ मुख्य नगर थे। इन नगरों की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
(a) मेसोपोटामिया के शहर आकार की दृष्टि से काफी विशाल थे। उदाहरण के लिए, उरुक शहर 2800 ई. पू. में लगभग 400 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था।
(b) मेसोपोटामिया के उरुर, उर, बेबीलोन तथा निनेवे जैसे शहरों की विशालता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सिन्धु घाटी के नगर हड़प्पा व मोहनजोदड़ों से भी कई गुणा बड़े थे।
(c) 331 ई. पू. (सिकन्दर के आक्रमण के समय) मेसोपोटामिया का बेबीलोन नगर 850 हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ था। मेसोपोटामिया के इन शहरों का आकार समय के साथ निरन्तर बड़ा होता गया।
(d) मंदिर इस सभ्यता के नगरों के केन्द्र-बिन्दु थे। प्रत्येक नगर का अपना देवता तथा उसका मंदिर होता था। नगर में सबसे ऊँचे स्थान पर मंदिर बनाया जाता था। नगर में मंदिर वाले क्षेत्र को ‘पवित्र क्षेत्र’ कहा जाता था।
(e) पवित्र क्षेत्र में बने मंदिर को पक्की ईंटों से बनाया जाता था, जिसे ‘जिगुरात’ कहा जाता था। जिगुरात का अर्थ था-स्वर्ग की पहाड़ी। इसी स्थल पर पुरोहित-राजा रहते थे तथा नगर की प्रशासन व्यवस्था का संचालन भी यहीं से होता था।
(f) मेसोपोटामिया के नगरों में नगर-नियोजन का सर्वथा अभाव था। यहाँ गलियाँ तंग व गंदगी से अटी होती थीं। गलियों की दशा का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भारी सामान गधों की सहायता से ही मकानों में पहुँचाया जा सकता था।
(g) घरों से जल-निकासी का प्रबंध भी न के बराबर था। वर्षा का पानी व गंदगी घरों में घुस जाती थी। घरों का पानी बाहर निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए गलियाँ कीचड़ व गंदगी से भरी रहती थीं।
(h) मकान प्रायः पक्की ईंटों के बने होते थे। गली का पानी आने से रोकने व कुछ धार्मिक विश्वासों के कारण मकान की दहलीज ऊँची बनाई जाती थी। मकानों में खिड़कियों की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। रोशनी प्रायः दरवाजों से ही आती थी।
(i) वर्षा के समय मकानों की छत का पानी गली की अपेक्षा घरों के अंदर ही गिरता था। इस पानी को आँगन में बने जल-हौज में एकत्रित किया जाता था।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि नगर-नियोजन की दृष्टि से मेसोपोटामिया के नगर समकालीन सिन्धु घाटी के नगरों के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। नगर-नियोजन की दृष्टि से सिन्धु घाटी इस सभ्यता से काफी विकसित थी।
प्रश्न8. “कालगणना, गणित, भवन-निर्माण व लेखन के लिए विश्व सदा मेसोपोटामिया सभ्यता का ऋणी रहेगा” कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए ।
अथवा
मेसोपोटामिया सभ्यता की वर्तमान विश्व को देन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।
उत्तर- मेसोपोटामिया सभ्यता के कालगणना, गणित, लेखन व भवन निर्माण के क्षेत्र में विश्व को बहुमूल्य देन दी है। उन्होंने एक विशेष प्रकार की लिपि (कीलाकार) का आविष्कार करके भाषा एवं साहित्य के सृजन में विशेष योगदान दिया। ज्ञान-विज्ञान, गणित व वास्तुकला में भी उन्होंने अपनी अनोखी प्रतिभा का परिचय दिया। आधुनिक विश्व सभ्यता के विकास में इस सभ्यता से अर्जित ज्ञान का महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस संदर्भ में मेसोपोटामिया की देन को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
- लेखन (Writing) – मेसोपोटामिया की लेखन पद्धति को सबसे महत्त्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ियों तक पहुँचाने में लेखन पद्धति का विशेष योगदान होता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सर्वप्रथम एक लिपि का आविष्कार किया, जिसे ‘कीलाकार’ कहा जाता था। इसलिए इस लिपि को मेसोपोटामियासभ्यता की सबसे बड़ी देन माना जाता है। इस लिपि के आविष्कार के परिणामस्वरूप ही आगे चलकर विश्व के अलग-अलग भागों में पाठशालाओं का उदय हुआ। इससे भाषा एवं शिक्षा के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। इस सभ्यता की लिपि में शुरू में 350 संकेत चिह्न थे, जो धीरे-धीरे संशोधित होकर घटते गए तथा अंततः 41 अक्षरों में सिमट गए।
- गणित (Mathematics)- यहाँ के लोगों ने गणित के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। इन लोगों को जोड़, घटा, गुणा, भाग, वर्गमूल तथा घनमूल का ज्ञान था। वे आज की तरह एक वृत्त को 360 अंशों में विभाजित करते थे। उनका सही ज्ञान आगे चलकर पाइथोगोरस के प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध îहुआ। यहाँ के लोगों द्वारा अपनाए गए 60 की संख्या के आधार पर ही बाद में समय की गणना में 60 मिनट का घण्टा तथा 60 सेकेंड का एक मिनट की इकाई का आरम्भ हुआ। उनकी इन सभी गणितीय उपलब्धियों का ज्ञान हमें 1800 ई. पू. से पहले की मिली कुछ पट्टिकाओं से होता है। ये लोग भार की इकाई के रूप में ‘मीना’ का प्रयोग करते थे, जो 60 शेकल के बराबर माना जाता था। उनकी गणितीय उपलब्धियों के लिए वर्तमान विश्व उनका सदा ऋणी रहेगा।
- कालगणना (Time Calculation) – कृषि की आवश्यकताओं ने इन लोगों में बहुत-सी विद्याओं को जन्म दिया। इन्हीं विद्याओं में एक कालगणना का ज्ञान भी मेसोपोटामिया के लोगों ने प्राप्त कर लिया था। उन्होंने दिन-रात की कल्पना से आगे बढ़कर चन्द्रमा के आधार पर महीनों की रचना की और सौरवर्ष की खोज की। उन्होंने चन्द्र पंचांग और सौर पंचांग के अन्तर को दूर करने के लिए अतिरिक्त मास की गणना का नियम बनाया। वे नक्षत्र और ग्रहों में अंतर को भी जानते थे। उन्होंने आकाश को अलग-अलग 12 भागों में बाँटा तथा उनका नामकरण किया। ये नाम आज भी प्रचलन में हैं। इनके चन्द्र पंचांग में 12 मास, चार सप्ताह और एक सप्ताह में 7 दिन होते थे। एक दिन 24 घण्टों में तथा घण्टा 60 मिनट में विभाजित होता था। समय की गणना का यह तरीका आज भी लगभग समान रूप से प्रचलित है। इसलिए मेसोपोटामिया की कालगणना विश्व को महत्त्वपूण् देन है।
- भवन-निर्माण (Architecture)- यहाँ के वास्तुकार स्तम्भों एवं मेहराबों का प्रयोग करना जानते थे। निप्पुर नगर की खुदाई में 3000 ई. पू. की मेहराबें प्राप्त हुई हैं। भवनों के अन्दर की दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था। भवनों के मध्य में हालनुमा एक बड़ा कमरा होता था। परन्तु उनकी मेहराब (हाट) बनाने की कला को सबसे अनोखा माना जाता है। इन मेहराबों से बने भवन सुंदर तथा मजबूत होते थे। आगे चलकर यह मेहराब बनाने की वास्तुकला काफी लोकप्रिय हुई।
उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीन विश्व की एक महानतम् सभ्यता थी। नगर एवं नगर-राज्यों के विकास की संकल्पना प्राचीन विश्व को उन्हीं की देन है। उन्होंने ही प्राचीनतम ‘कीलाकार’ लिपि का आविष्कार करके विश्व को बौद्धिक प्रगति के पथ पर चलना सिखाया। विधि-संहिताओं का निर्माण करके उन्होंने समाज को कानूनी रूप से सुदृढ़ किया। मेहराव, गुम्बद, स्तम्भ व कुम्हार के चाक के प्रथम आविष्कारकर्ता भी यही थे। अंततः कहा जा सकता है कि वर्तमान विश्व सदा उसकी देन के लिए उसका ऋणी रहेगा।
लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर
प्रश्न 1. मेसोपोटामिया के भौगोलिक विभाजन व क्षेत्र विशेष की भाषा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए ।
उत्तर- अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश के भौगोलिक विभाजन व उससे संबंधित भाषा के विविध पहलू निम्न हैं-
(1) मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को मुख्यतः सुमेर और अक्कद कहा जाता था।
(2) 2000 ई. पू. के बाद जब बेबीलोन शहर का विकास हुआ तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा।
(3) 1100 ई. पू. में मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में असीरियाइयों द्वारा अपना राज्य स्थापित किया गया। इसके बाद इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा।
(4) सभ्यता के आरंभिक चरण में सुमेरी भाषा का बोलबाला था, परन्तु 2400 ई. पू. के आसपास इस भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने लिया था। यह भाषा सिकन्दर के आक्रमण के समय (336-323 ई पू.) तक फलती-फूलती रही।
(5) अरामाइक भाषा का प्रवेश लगभग 1400 ई पू. में हुआ। यह भाषा हिब्रू जैसी थी तथा 1000 ई. पू. के आसपास अधिकतर क्षेत्र में इस भाषा का बोलबाला हो गया था। इराक के कुछ भागों में आज भी इस भाषा को बोला जाता है।
प्रश्न 2. ‘श्रम-विभाजन’ किस प्रकार शहरी जीवन की विशेषता होती है?
उत्तर- जब किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ने लगती हैं, उस स्थान पर जनसंख्या का घनत्त्व बढ़ने लगता है, लोगों को वहाँ रहना सुविधाजनक लगता है, तब कस्बों का निर्माण होता है। आगे चलकर यही कस्बे शहर का रूप धारण करते हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार, उत्पादन और भिन्न-भिन्न प्रकार की अन्य सेवाओं की भी उपयोगी भूमिका होती है। इस दृष्टि से शहरों के लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकते है। उन्हें ग्रामीण उत्पादन या उनके द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए उन पर निर्भर होना पड़ता है। उनके बीच लेन-देन निरन्तर होता रहता है। उदाहरण के लिए, काँसे के औजार बनाने वाला धातु-तांबा या टिन लाने के स्वयं बाहर नहीं जाता है। उसे ईंधन के रूप में कोयला भी दूसरे लोग ही उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर को भी औजार और पत्थर भी अन्य लोगों द्वारा ही उपलब्ध करवाए जाते हैं। कारीगर की विशेषज्ञता तो मात्र नक्काशी अर्थात् पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। संबंधित वस्तु के व्यापार से भी उसका अधिक संबंध नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि श्रम-विभाजन शहरी जीवन की मूलभूत आवश्यकता होता है।
प्रश्न 3. मेसोपोटामियाई लोगों के आयात-निर्यात के विषय में आप क्या जानते हो?
उत्तर- मेसोपोटामिया खाद्य पदार्थों की दृष्टि से काफी सम्पन्न था, परन्तु वहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। इसलिए उन्हें दूसरे क्षेत्रों से इन्हें प्राप्त करना पड़ता था तथा बदले में अपना कुछ सामान उन्हें देना पड़ता था। मेसोपोटामिया के आयात-निर्यात के विभिन्न पहलुओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
(1) इस सभ्यता के लोगों को मोहरें, आभूषण और औजार बनाने के लिए अच्छा पत्थर बाहर से मंगवाना पड़ता था, क्योंकि इनके यहाँ इस तरह के पत्थरों की कमी थी।
(2) गाड़ियाँ व उनके पहिए तथा नाव बनाने के लिए भी उन्हें अच्छी लकड़ी बाहर से मंगवानी पड़ती थी। खजूर और पोपलार की लकड़ी जो इनके यहाँ होती थी, वह इस कार्य के लिए उपयुक्त न थी।
(3) औजार, पात्र व गहने बनाने के लिए धातु भी बाहर से मंगवानी पड़ती थी।
(4) संभवतः सोना, चाँदी, ताँबा, टिन, सीपी व लकड़ी व विभिन्न प्रकार के पत्थर वे तुर्की और ईरान से मंगवाते थे।
(5) उपरोक्त चीजों को प्राप्त करने के लिए वे अपना कपड़ा तथा कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते थे।
प्रश्न 4. मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही में जलमार्गों का क्या महत्त्व था?
उत्तर- शहरी विकास के लिए सस्ती, सरल व सुगम परिवहन व्यवस्था का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। बैलगाड़ियों में या पशुओं की पीठ पर रखकर भारी सामान को इधर-उधर ले जाना आसान नहीं होता है। इस तरह की आवाजाही में समय ज्यादा लगता है तथा पशुओं के रख-रखाव पर खर्चा भी अधिक होता है। सही मायनों में शहरी अर्थव्यवस्था का बोझ इस तरह के परिवहन साधनों से नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता और अच्छा साधन जलमार्ग ही होता है। इस तरह के जलमार्गों से भारी से भारी सामान बिना खर्चे के आसानी से इधर से उधर भेजा जा सकता है। भारी सामान से लदी नावें नदी की धारा या हवा की गति से अपने आप चलती हैं। इस दृष्टि से प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएँ छोटी-बड़ी बस्तियों के बीच माल की आवाजाही का सबसे अच्छा माध्यम थीं। इन नहरों और प्राकृतिक जलधाराओं के माध्यम से ही मेसोपोटामिया के लोग स्थानीय व विदेशी व्यापार का संचालन करते थे। जलमार्ग की दृष्टि से मेसोपोटामिया की ‘फरात’ नदी ‘विश्व-मार्ग’ के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के शहरों में माल की आवाजाही में जलमार्गों का विशेष महत्त्व था।
प्रश्न 5. मेसोपोटामिया की मूर्तिकला को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- कला की दृष्टि से भी मेसोपोटामिया की सभ्यता महान थी। इसके ऊरक नगर से प्राप्त एक स्त्री के सिर की मूर्ति इसका स्पष्ट प्रमाण है। यह लगभग 3000 ई. पू. की है। इस प्राप्त मूर्ति का गहराई से अध्ययन करने पर हमें मेसोपोटामिया की मूर्ति कला के बारे में निम्न बातें पता चलती हैं-
(1) इस मूर्ति में स्त्री का जो सिर दिखाई देता है, उसको सफेद संगमरमर से तराश कर बनाया गया है।
(2) इसकी आँखों और भौंहों में क्रमशः नीले लाजवर्द, सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी।
(3) इस मूर्ति के माथे के ऊपर एक खाँचा बना हुआ है, शायद यह गहना पहनने के लिए बनाया होगा।
(4) इसके मुख, होठों, ठोड़ी और गालों की सुकोमल-सुंदर बनावट देखते ही बनती है।
(5) इस मूर्ति को बनाने में कठोर पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस तरह का पत्थर मेसोपोटामिया में नहीं था। इसलिए इसे शायद बाहर से मंगवाया होगा।
(6) यह मूर्तिकला का एक विश्व-प्रसिद्ध नमूना है। इस मूर्ति की उपरोक्त विशेषताएँ मेसोपोटामिया की मूर्तिकला की ही विशेषताएं मानी जा सकती हैं।
प्रश्न 6. मेसोपोटामिया सभ्यता में जिगुरात के निर्माण की प्रक्रिया उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए ।
उत्तर- मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर नगर-राज्यों में जिगुरात (मंदिर) का विशेष महत्त्व था। इनके महत्त्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके पुरोहित राजा का निवास स्थल इनमें ही होता था। इनको बनाने के लिए अत्यधिक श्रम व संसाधनों की आवश्यकता होती थी। उरुक नगर के एक मंदिर (जिगुरात) की निर्माण-प्रक्रिया से इसे आसानी से समझा जा सकता है। उरुक एक मंदिर केन्द्रित राज्य था तथा 2800 ई. पू. के आसपास यह 400 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक सुदृढ़ प्राचीर का निर्माण किया गया था। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर से संबंधित काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही न देना पड़े, परन्तु इन मंदिरों में उन्हें काम अवश्य करना पड़ता था। काम के बदले वेतन की अपेक्षा अनाज आबंटित किया जाता था। इस नगर के एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 व्यक्तियों ने लगभग पाँच साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। मंदिर के लिए पत्थर खोदने, धातु-खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करना व मंदिर में लगाना तथा बाहर से मंदिर के लिए जरूरी सामान लाना कुछ ऐसे कार्य थे, जिन्हें आम लोगों को करना होता था। सैकड़ों लोग चिकनी मिट्टी के शंकु (कोन) बनाने, इनमें रंग भरने और फिर इन्हें दीवारों पर लगाने में लगे होते थे। बाहर से मंगवाए गए पत्थरों की मूर्ति बनाकर इन्हें मंदिरों में लगाने का काम भी शासक की देखरेख में होता था।
प्रश्न 7. जिमरीलिम का मारी स्थित राजमहल क्यों विशेष था?
उत्तर- 1810-1760 ई. पू. में मारी नगर-राज्य में राजा जिमरीलिम का राजमहल कई कारणों से विशेष था, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
(1) यह विशाल राजमहल शाही परिवार का निवास स्थल था। प्रशासन का केन्द्र-बिन्दु भी यही महल था।
(2) कीमती धातुओं के आभूषणों का निर्माण भी इसी राजमहल की कार्यशाला में होता था।
(3) राजा के भोजन की मेज पर प्रतिदिन भारी मात्रा में रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा व बीयर पेश किए जाते थे। इससे इसकी भव्यता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।
(4) राजा सफेद पत्थर जड़े आंगन पर बैठकर भोजन करता था। उसके साथी भी उसके साथ भोजन करते थे।
(5) महल का प्रवेश द्वार, विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से अलंकृत थे। इसे देखने दूर-दूर से लोग आते थे।
(6) यह महल लगभग 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था तथा इसमें 260 कमरे थे।
प्रश्न 8. “मारी नगर व्यापार और समृद्धि के मामले में अद्वितीय था” कथन को स्पष्ट कीजिए।
उत्तर- मारी नगर की व्यापारिक समृद्धि को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-उत्तर-
(1) यह नगर बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से बहुत मात्रा में आयात-निर्यात होता था।
(2) यहाँ से फरात नदी के रास्ते दक्षिणी भाग, तुर्की, सीरिया और लेबनान जैसे दूर-दराज क्षेत्रों से व्यापार होता था।
(3) दक्षिण नगरों से आने वाले मालवाहक जलपोतों का ठहराव भी यहीं होता था। इसके बदले उनसे कुल माल मूल्य का 10 प्रतिशत कर वसूला जाता था।
(4) साइप्रस के द्वीप ‘अलाशिया’ से होने वाले ताँबे तथा टिन के व्यापार पर भी इसी शहर का व्यापारिक नियन्त्रण था।
(5) मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए। शहरीकेन्द्र का एक अच्छा उदाहरण है। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया का मारी नगर व्यापार और समृद्धि के मामले में अद्वितीय था।
प्रश्न 9. वेबीलोन नगर की मुख्य विशेषताओं पर संक्षिप्त में प्रकाश डालिए।
उत्तर- बेबीलोनिया को 625 ई. पू. में शूरवीर शासक नैबोपोलास्सर ने असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवाया था। उसने तथा उसके उत्तराधिकारियों ने 331 ई. पू. (सिकन्दर का आक्रमण) तक बेबीलोन को दुनिया का एक प्रमुख नगर बना दिया था। इस नगर की मुख्य विशेषताओं को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
(1) यह नगर 850 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था।
(2) इसकी चारदीवारी तिहरी थी तथा इसमें बड़े-बड़े राजमहल तथा मंदिर विद्यमान थे।
(3) इसमें एक जिगुरात अर्थात् सीढ़ीदार मीनार भी थी तथा इसके मुख्य देवस्थल तक जाने के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था।
(4) इसके व्यापारिक घराने स्वयं व्यापार में रुचि रखते थे तथा दूर-दूर तक अपना करोगार करते थे।
(5) यहाँ के गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थीं, जो आने वाले समय के लिए इनकी महानतम देन हैं।
प्रश्न 10. मेसोपोटामिया के धार्मिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर- मेसोपोटामिया के लोगों का अनेक देवी-देवताओं में विश्वास था। उनमें शमाश (सूर्य देवता), उर (चन्द्र देवता), इन्नाना (प्रेम व युद्ध की देवी), अनु (आकाश का देवता), एनालील (वायु देवता) आदि प्रमुख थे। बेबीलोन के निवासी विशेष रूप से ‘मार्दुक’ और असीरिया के लोग ‘अस्सुर’ नामक देवता की उपासना करते थे। इस सभ्यता के प्रत्येक नगर में एक प्रधान मन्दिर होता था। वहाँ का देवता नगर का संरक्षक माना जाता था। नगर के संरक्षक देवता के लिए नगर के ‘पवित्र क्षेत्र’ में किसी पहाड़ी या ईंटों के बने चबूतरे पर मन्दिर का निर्माण किया जाता था, जिसे ‘जिगुरात’ कहते थे। लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़-बकरी आदि पशुओं की बलि चढ़ाते थे। उनकी पूजा स्वार्थ-प्रेरित होती थी। उसमें श्रद्धा का अभाव पाया जाता था। उनका विश्वास था कि देवी-देवताओं को प्रसन्न रखकर ही भौतिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। वे अन्धविश्वासी थे तथा जादू-टोनों व भूत-प्रेत में बहुत विश्वास रखते थे। बाढ़, अकाल तथा महामारी को वे देवता का प्रकोप मानते थे। इस सभ्यता के लोग परलोक के स्थान पर इस लोक की चिन्ता अधिक करते थे। उनका विश्वास था कि परलोक अन्धकार और दुर्भिक्ष (अकाल) का डेरा है, जहाँ पेट भरने के लिए केवल मिट्टी मिलती है।
प्रश्न 11. मेसोपोटामियाई समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी?
उत्तर– इस समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। दहेज से प्राप्त सम्पत्ति पर स्त्री का अधिकार होता था। उसकी इच्छा से पुरुष उस सम्पत्ति का अधिकारी हो सकता था। पति तथा पुत्र के न होने की स्थिति में परिवार की सम्पत्ति में स्त्री का भी अधिकार माना जाता था। पत्नी को अपने पति से अलग स्वतन्त्र रूप से व्यापार करने एवं दासियाँ रखने का भी अधिकार था। इसके विपरीत समाज में स्त्रियों पर कुछ प्रतिबंध भी थे। उससे अपने पति के लिए कई सन्तान उत्पन्न करने की अपेक्षा की जाती थी। बांझपन की स्थिति में उसे तलाक भी दिया जा सकता था। व्यभिचारी स्त्री को मृत्युदण्ड दिए जाने का प्रावधान था। देवदासी प्रथा का प्रचलन भी था अर्थात् सुन्दर युवतियों को मंदिरों में देवता की सेवा के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता था। जब परिवार की किसी लड़की को मंदिर में समर्पित किया जाता था, तो उस समय परिवार में उत्सव मनाया जाता था। इस अवसर पर लड़की की शादी में दिया जाने वाला दहेज उसे भेंट में दिया जाता था।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मेसोपोटामिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर– दजला और फरात नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। शहरी जीवन की शुरूआत इसी प्रदेश से हुई भी। यह सभ्यता अपनी समृद्धि, सम्पन्नता, शहरी जीवन, लेखन पद्धति, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित तथा खगोलविद्या के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है।
प्रश्न 2. मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसके साहित्य का क्षेत्रीय फैलाव कैसे हुआ?
उत्तर-2000 ई. पू. के बाद इस सभ्यता की लेखन प्रणाली व साहित्य का फैलाव पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेशों, उत्तरी सीरिया, तुर्की तथा मिस्र तक हुआ था। इन प्रदेशों में इस सभ्यता की भाषा तथा लिपि का प्रचलन सामान्य हो गया था।
प्रश्न 3. मेसोपोटामिया सभ्यता के मुख्य केन्द्र कौन-से थे?
उत्तर-इस सभ्यता का क्षेत्र केवल दजला व फरात नदियों के मध्य तक सीमित न होकर फारस की खाड़ी के दक्षिण तक विस्तृत था। इस क्षेत्र को तीन प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्रथम-दजला व फरात के बीच का क्षेत्र (दोआब) जिसको सीरिया कहा जाता है, दूसरा संगम से सटा क्षेत्र अक्कद तथा तीसरा-सुमेर।
प्रश्न 4. मेसोपोटामिया सभ्यता के अन्तर्गत आने वाली सभ्यताओं के नाम लिखो।
उत्तर-मेसोपोटामिया के तीन क्षेत्रों (सीरिया, अक्कद व सुमेर) में प्राचीन काल में चार सभ्यताएँ विकसित हुईं, जिन्हें असीरियन, कैल्डीयन, बेबीलोनियन तथा सुमेरियन के नाम से जाना जाता है। इन सभ्यताओं में सबसे पहले ‘सुमेरियन’ सभ्यता का विकास हुआ ।
प्रश्न 5. मेसोपोटामिया सभ्यता में भाषा विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
उत्तर-इस सभ्यता की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ई. पू. में इस भाषा का स्थान अक्कदी भाषा ने ले लिया। सिकन्दर के समय (336 323 ई. पू.) तक यह भाषा कुछ परिवर्तनों के साथ फलती-फूलती रही। 1400 ई. पू. में हिब्रू भाषा से मिलती-जुलती अरामाइक भाषा का प्रवेश इस प्रदेश में हुआ तथा 1000 ई. पू. के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में यह बोली जाती है।
प्रश्न 6. यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्त्वपूर्ण था?
उत्तर- यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया दो कारणों से बड़ा महत्त्वपूर्ण था-
(i) बाईबल के प्रथम भाग ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ में इसके शहर ‘शिमार’ अर्थात् ‘सुमेर’ का जिक्र है तथा इसे ईंटों से बना शहर बताया गया है।
(ii) यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे।
प्रश्न 7. बाईबल में दी गई ‘जलप्लावन’ की विषय वस्तु क्या है?
उत्तर- बाईबल के अनुसार ‘जलप्लावन’ की घटना पृथ्वी पर सम्पूर्ण जीवन को नष्ट करने वाली थी। परन्तु परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रखने के लिए ‘नोआ’ नामक मनुष्य का चुनाव किया। नोआ ने विशाल नाव पर सभी जीव-जंतुओं का एक-एक जोड़ा रख लिया और जलप्लावन से इन्हें सुरक्षित बचाया। इनको छोड़कर बाकी सब कुछ इसमें नष्ट हो गया।
प्रश्न 8. क्या मेसोपोटामिया सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी?
उत्तर- मेसोपोटामिया में प्राचीन नगरों का निर्माण 3000 ई. पू. में शुरू हो गया था। इस काल को इतिहास में कांस्य युग की संज्ञा दी जाती है। काँसा तांबे व टिन के मिश्रण से बनता है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अधिकतर औजार, बर्तन व आभूषणों में इसी धातु का प्रयोग हुआ है। इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है।
प्रश्न 9. श्रम-विभाजन की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है?
उत्तर- शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त व्यापार, उत्पादन और तरह-तरह की सेवाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई एक व्यक्ति इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए उसे इसके लिए भिन्न-भिन्न लोगों की सेवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। इस तरह के कार्य बंटवारे को ही श्रम-विभाजन की संज्ञा दी जाती है। शहरी-जीवन इसी अवधारणा पर टिका होता है।
प्रश्न 10. मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की क्या स्थिति थी?
उत्तर- इस सभ्यता में खनिज संसाधनों का अभाव था। इसके दक्षिणी भाग में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इसके अतिरिक्त मजबूत नाव बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का भी अभाव था। औजार, पात्र व गहने बनाने के लिए भी धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। लकड़ी, तांबा, राँगा, चाँदी, सोना, सीपी व पत्थर वे बाहर से मंगवाते थे।
प्रश्न 11. लेखन कार्य की शुरूआत किन परिस्थितियों में हुई?
उत्तर- जब तत्कालीन समाज को लेन-देन का स्थायी हिसाब-किताब रखने की जरूरत पड़ी, तब शायद लेखन कार्य की शुरूआत हुई। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण था, क्योंकि शहरी जीवन में लेन-देन अलग-अलग समय पर तथा अलग-अलग लोगों द्वारा किए जाते थे। इसलिए इसके हिसाब-किताब के लिए ही लेखन कार्य की शुरूआत हुई।
प्रश्न 12. मेसोपोटामिया की प्राचीनतम पट्टिकाओं (Tablet) के विषय में आप क्या जानते हो?
उत्तर- मेसोपोटामिया से प्राप्त प्राचीनतम पट्टिकाएँ लगभग 3200 ई. पू. की हैं। इन पर चित्र जैसे चिह्न व संख्याएं दी गई हैं। लगभग 5000 पट्टिकाएँ ऐसी मिली हैं, जिन पर बैलों, मछलियों और रोटियों के चिह्न हैं। ये चिकनी मिट्टी से बनी तथा धूप में पकाई गई हैं। प्रत्येक पट्टिका की ऊँचाई 3.5 सेमी. या उससे कम है।
प्रश्न 13. लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता क्यों होती थी?
उत्तर- मेसोपोटामिया सभ्यता के समय किसी भाषा-विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप से प्रस्तुत करना कतई आसान न था। इसके लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती थी। इसे बहुत कम लोग ही कर पाने में सक्षम थे। इसलिए उस समय मेसोपोटामिया में कहावत प्रचलित थी, “जो लेखन-पद्धति में प्रवीण होगा, वह सूर्य की तरह चमकेगा।”
प्रश्न 14. मेसोपोटामियाई महाकाव्य के अनुसार पट्टिकाएं लिखने की शुरूआत किस प्रकार हुई थी?
उत्तर- महाकाव्य के अनुसार उरुक के प्राचीन शासक एनमर्कर ने अपने एक दूत को अपने संदेश के साथ अरट्टा के मुखिया के पास भेजा, परन्तु उसने राजा के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमर्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उस समय मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। महाकाव्य के अनुसार इस तरह पट्टिकाएं लिखने की शुरूआत हुई।
प्रश्न 15. मेसोपोटामिया में शुरूआती मंदिरों का स्वरूप कैसा था?
उत्तर- लगभग 5000 ई. पू. में दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इसमें से कुछ ने शहरों का रूप ले लिया। इसी समय कच्ची ईंटों से मंदिर बनाने की प्रथा का आरम्भ हुआ। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटे-से देवालय जैसा है। देवता पूजा का केन्द्र-बिन्दु होता था। लोग देवी-देवता को अन्न, दही व मछली का चढ़ावा चढ़ाते थे।
प्रश्न 16. शहरी अर्थव्यवस्था के लिए चाक का निर्माण किस तरह महत्त्वपूर्ण था?
उत्तर- सम्भवतः चाक पर बर्तन बनाने की कला का विकास मेसोपोटामिया सभ्यता के काल में ही हुआ था। यह शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हुआ। इस चाक के निर्माण से कुम्हार की कार्यकुशलता पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई। अब वह एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बना सकता था।
प्रश्न 17. मेसोपोटामियाई समाज में विवाह की रस्म किस प्रकार सम्पन्न की जाती थी?
उत्तर- वर की इच्छा के बाद वधू के माता-पिता विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष को उपहार दिए जाते थे। इसके बाद दोनों परिवार (वर व वधू) एक साथ बैठकर भोजन करते थे। मंदिर में भेंट चढ़ाने के बाद नववधू की सास उसे लेने आती थी। इस तरह उस समय विवाह की रस्म सम्पन्न होती थी।
प्रश्न 18. मेसोपोटामियाई समाज में वास्तुकला संबंधी किस तरह के शकुन-अपशकुन प्रचलित थे?
उत्तर- इन शकुन-अपशकुन संबंधी बातों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है-
(i) जिस घर की दहलीज ऊँची होती है, वहाँ धन-दौलत आती है।
(ii) सामने का दरवाजा यदि किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है।
(iii) अगर घर का मुख्य दरवाजा भीतर की अपेक्षा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी।
प्रश्न 19. मेसोपोटामिया की शवाधान विधि क्या थी?
उत्तर- मेसोपोटामिया की शवाधान विधि के लक्षण निम्न हैं-
(i) उर में नगरवासियों के लिए कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जन-साधारण को दफनाया जाता था।
(ii) कुछ शव साधारण घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए हैं।
प्रश्न 20. मेसोपोटामिया नगर बनने से पहले ‘मारी’ का स्वरूप कैसा था?
उत्तर- मारी फरात नदी की उर्ध्वधारा पर स्थित है। इस क्षेत्र में कृषि तथा पशुपालन का कार्य साथ-साथ होता था। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भेड़-बकरी चराने के ही काम आता था। यहाँ के पशु चारकों को जब किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता होती थी, तब वे अपने पशुओं और उनके पनीर, चमड़ा व माँस आदि के बदले में वे चीजें प्राप्त करते थे। यही मारी 2000 ई. पू. के बाद शाही राजधानी के रूप में खूब फला-फूला।
प्रश्न 21. मारी शहर के किसानों और खानाबदोश गड़रियों के बीच किस बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता था?
उत्तर- इनके बीच निम्न बातों को लेकर झगड़ा होता था-उत्तर-
(i) खानाबदोश गड़रिए किसान के बोए हुए खेत से अपनी भेड़-बकरियों को गुजार कर ले जाते थे। इससे किसान की फसल को नुकसान होता था।
(ii) कई बार खानाबदोश गड़रिए किसानों के गांवों पर हमला करके उनका एकत्रित किया हुआ माल लूट ले जाते थे।
प्रश्न 22. क्या मेसोपोटामिया की सभ्यता में यायावर समुदाय का अस्तित्त्व था?
उत्तर- मेसोपोटामिया के मुख्य भूमि प्रदेश (दक्षिणी) में यायावर समुदायों के झुंड के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये समूह गड़रिए, मजदूरों तथा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, ऐमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति से संबंधित थे। इनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन भी स्थापित कर लिया था।
प्रश्न 23. आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मन्दिर घर जैसे ही रहे होंगे?
उत्तर- ऐसा सोचने के निम्न कारण हैं-
(i) पुराने मन्दिरों का आकार बहुत छोटा है तथा इनकी बनावट भी घरों जैसी है।
(ii) इन्हें (मंदिर) भी घरों की तरह कच्ची ईंटों से बनाया गया था।
(iii) इनमें भी घरों की तरह आँगन होता था, जिसके चारों ओर बरामदे और कमरे बने होते थे।
प्रश्न 24. ‘पेपर’ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई?
उत्तर- शुरूआती लेखन पेड़ों के पत्तों पर या उनकी छाल पर किया जाता था। मिस्र में लगभग 3000 ई. पू. में ‘पेपिरस’ नामक पेड़ के पत्तों पर सरकंडे की सहायता से लेखन का कार्य होता था। इसी पेपिरस से आगे चलकर अंग्रेजी भाषा का शब्द ‘पेपर’ बना। हिन्दी भाषा का कागज शब्द इसी का रूपांतरित शब्द है।
प्रश्न 25. क्या मेसोपोटामियाई समाज में एकल परिवार की अवधारणा विकसित हो चुकी थी?
उत्तर- मेसोपोटामिया में एकल परिवार की अवधारणा पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। उस समय के कानूनी दस्तावेजों से पता चलता है कि एकल परिवार को आदर्श परिवार माना जाता था। इस तरह के परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी व उनके बच्चे शामिल होते थे। परिवार का मुखिया पिता होता था।
बहु-विकल्पीय प्रश्नोत्तर
- मेसोपोटामिया की ज्ञात सबसे प्राचीन भाषा थी-
(A) अक्कदी (B) अरामाइक (C) हिब्रू (D) सुमेरियन
उत्तर- (D) सुमेरियन
- मेसोपोटामिया सभ्यता थी-
(A) ताम्रयुगीन (B) कांस्ययुगीन (C) लौहयुगीन (D) उपरोक्त सभी
उत्तर-(B) कांस्ययुगीन
- शहरी जीवन की शुरूआत हुई थी-
(A) मेसोपोटामिया से (B) हड़प्पा से (C) मोहनजोदड़ो से (D) मिस्र से
उत्तर- (A) मेसोपोटामिया से
- दजला और फरात नदियों के मध्य का क्षेत्र वर्तमान में निम्न का एक भाग है-
(A) ईरान का (B) मिस्र का (C) ईराक का (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (C) ईराक का
- मेसोपोटामिया सभ्यता निम्न के लिए प्रसिद्ध है-
(A) शहरी जीवन (B) लेखन पद्धति (C) खगोल विद्या (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी
- मेसोपोटामिया नाम निम्न भाषा के शब्दों के मेल से बना है-
(A) यूनानी (B) अरबी (C) फारसी (D) अंग्रेजी
उत्तर- (A) यूनानी
7. ‘ओल्ड टेस्टामेंट’ निम्न धार्मिक ग्रन्थ का भाग है-
(A) गीता (B) कुरान (C) बाईबल (D) जेथुइट
उत्तर- (C) बाईबल
8. अक्कदी भाषा ने कब सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था?
(A) 2400 ई. पू. में (B) 3200 ई. पू. में
(C) 5200 ई. पू. में (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) 2400 ई. पू. में
9. मेसोपोटामिया के किस भाग में सर्वप्रथम शहरों का उदय हुआ था ?
(A) दक्षिणी भाग बेबीलोन में (B) दक्षिणी भाग अक्कद में
(C) (A) और (B) दोनों (D) दक्षिणी भाग सुमेर में
उत्तर- (D) दक्षिणी भाग सुमेर में
10. मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से संबंध रखने वाले क्षेत्र-
(A) सुमेर (B) अक्कद (C) बेबीलोन (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी
11. मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग से संबंध रखने वाली सभ्यता थी-
(A) सुमेर (B) बेबिलोनिया (C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (C) (A) और (B) दोनों
12. असीरियाइयों ने मेसोपोटामिया के किस भाग में अपना राज्य स्थापित किया था?
(A) उत्तर (B) पूर्व (C) दक्षिण (D) पश्चिम
उत्तर- (A) उत्तर
13. वाईबल के अनुसार परमेश्वर ने जलप्लावन से सृष्टि को बचाने के लिए किस मनुष्य का चुनाव किया?
(A) नोआ (C) कौना (B) सेवा (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) नोआ
14. मेसोपोटामिया के परम्परागत साहित्य में जलप्लावन की घटना का नायक किसे बताया गया है?
(A) जिउसूद्र (B) नोआ (C) सेवा (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) जिउसूद्र
15. मेसोपोटामिया का कौन-सा भाग रेगिस्तान था परन्तु फिर भी काफी उपजाऊ था?
(A) उत्तरी (B) पूर्वी (C) दक्षिणी (D) पश्चिमी
उत्तर- (C) दक्षिणी
16. मेसोपोटामिया के निम्न भाग में सबसे पहले नगरों व लेखन-प्रणाली का उदय हुआ था-
(A) पूर्वी (B) दक्षिणी (C) उत्तरी (D) पश्चिमी
उत्तर- (B) दक्षिणी
17. काँसा धातु निम्न के मिश्रण से तैयार की जाती थी-
(A) ताँवा व टिन (B) ताँबा व लोहा
(C) लोहा व टिन (D) इसमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) ताँबा व टिन
18. मेसोपोटामिया का व्यापार मुख्यतः निम्न मार्ग से होता था-
(A) जलमार्ग (B) स्थल मार्ग
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) जलमार्ग
19. मेसोपोटामिया की शुरूआती पट्टिकाएँ कितने ई. पू. की हैं?
(A) 5400 (B) 3600 (C) 4800 (D) 3200
उत्तर- (D) 3200
20. खानाबदोश लोगों का संबंध निम्न जाति से था-
(A) अक्कदी (B) ऐमोराइट और असीरियाई
(C) आर्मीनियन (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी
21. मारी नगर-राज्य के राजा निम्न समुदाय से थे-
(A) अक्कदी (B) ऐमोराइट (C) सुमेरी (D) असीरियाई
उत्तर- (B) ऐमोराइट
22. मेसोपोटामियाई पट्टिकाओं पर निम्न चिह्न या संकेत मिले हैं-
(A) मछली (B) नाव (C) बैल (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी
23. मेसोपोटामिया के लोग लिखते थे-
(A) ताड़-पत्र पर (B) पेपिरस-पत्र पर
(C) पट्टिकाओं पर (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (C) पट्टिकाओं पर
24. क्यूनीफार्म (कीलाकार) निम्न भाषा का शब्द है-
(A) यूनानी (B) लातिनी (C) हिब्रू (D) सुमेरियन
उत्तर- (B) लातिनी
25.मेसोपोटामिया का सबसे ज्ञात प्राचीन मंदिर है-
(A) 2400 ई. पू. में (B) 3200 ई. पू. में
(C) 2800 ई. पू. में (D) 5000 ई. पू. में
उत्तर- (D) 5000 ई. पू. में
26. मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास शुरू हुआ-
(A) 5000 ई. पू. का (B) 2400 ई. पू. का
(C) 3600 ई. पू. का (D) 4200 ई. पू. का
उत्तर- (A) 5000 ई. पू. का
27. ‘स्टेपी’ क्षेत्र के देवता थे-
(A) उर (B) उलुस (C) इन्नाना (D) ड्रैगन
उत्तर- (D) ड्रैगन
28. मेसोपोटामिया के लोग ‘अलाशिया’ द्वीप से निम्न वस्तु का आयात करते थे-
(A) ताँबा (B) टिन (C) (A) और (B) दोनों (D) लोहा
उत्तर- (C) (A) और (B) दोनों
29. ‘गिल्गेमिश’ महाकाव्य का संबंध है-
(A) हड़प्पा सभ्यता से (B) मेसोपोटामिया सभ्यता से
(C) मिस्र सभ्यता से (D) यूनानी सभ्यता से
उत्तर- (B) मेसोपोटामिया सभ्यता से
30. 2800 ई पू. के आसपास उरुक नगर का क्षेत्रफल था-
(A) 200 हेक्टेयर (B) 250 हेक्टेयर
(C) 300 हेक्टेयर (D) 400 हेक्टेयर
उत्तर- (D) 400 हेक्टेयर
31. गिल्गेमिश महाकाव्य का नायक निम्न नगर-राज्य का शासक था-
(A) अलाशिया (B) मारी (C) उरुक (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (C) उरुक
32. पत्थर के ऐसे शिलापट्ट जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे, कहा जाता था-
(A) स्टेल (B) फ्लीकर (C) स्टोन (D) सरकंडा
उत्तर- (A) स्टेल
33. मारी नगर कब शाही राजधानी के रूप में उभरा ?
(A) 1500 ई. पू. के बाद (B) 720 ई. पू. के बाद
(C) 1000 ई. पू. के बाद (D) 2000 ई. पू. के बाद
उत्तर- (D) 2000 ई. पू. के बाद
34. अंतिम असीरियाई शासक असुरवनिपाल (668-627 ई. पू.) ने कहाँ एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की?
(A) निनवै में (B) कालसट में (C) सहतर में (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) निनवे में
35. स्वतन्त्र बेबीलोन का अंतिम शासक था-
(A) सिकन्दर (B) नैबोनिडस (C) नैबोपोलास्सर (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (B) नैवोनिडस
36. सुमेरियन भाषा की लिपि थी-
(A) कीलाकार (B) अरामाइक (C) हिब्रू (D) अक्कदी
(C) (A) और (B) दोनों
उत्तर- (A) कीलाकार
37. निम्न नगर व्यापार के बल पर समुद्र नगर बना-
(A) मारी (B) टोकन (C) उरुक (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (A) मारी
38. प्रेम व युद्ध की देवी थी-
(A) इल्लाना (B) इन्नाना (C) उल्लेना (D) कल्लेना
उत्तर- (B) इन्नाना
39. मेसोपोटामिया सभ्यता में चन्द्र देवता था-
(A) उलुस (B) उर (C) इन्नस (D) शमाश
उत्तर- (B) उर
40. मेसोपोटामिया के लोग अपने देवताओं को निम्न भेंट चढ़ाते थे-
(A) मछली (B) दही (C) अन्न (D) उपरोक्त सभी
उत्तर- (D) उपरोक्त सभी
41. बेबीलोनिया का शाब्दिक अर्थ-
(A) मूर्तद्वार (B) कोमलद्वार (C) (A) और (B) दोनों (D) देवद्वार
उत्तर- (D) देवद्वार
42. सुमेर की सभ्यता में निम्न पंचांग प्रचलन में था-
(A) चन्द्र पंचांग (B) सूर्य पंचांग
(C) (A) और (B) दोनों (D) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (A) चन्द्र पंचांग
43. मेसोपोटामिया में लोहे के प्रयोग की शुरूआत हुई-
(A) 2300 ई. पू. में (B) 1000 ई. पू. में
(C) 3200 ई. पू. में (D) 2800 ई. पू. में
उत्तर- (B) 1000 ई. पू. में
44. निम्न में से कौन-सा नगर मेसोपोटामिया से संबंधित नहीं है?
(A) उर (B) मारी (C) कालीबंगन (D) पेट्सी
उत्तर- (D) पेट्सी
महत्त्वपूर्ण बिन्दु
० मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ दो नदियों के बीच का भाग होता है।
० प्राचीन इराक के दजला व फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था।
० कांस्य काल के इस क्षेत्र में सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन एवं कैल्डीयन सभ्यताओं का विकास हुआ।
० इस क्षेत्र में विकसित होने वाली प्रथम सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी।
० सुमेरियन सभ्यता एक नगर राज्यीय सभ्यता थी, जिसके प्रमुख नगर उर, एरिडु, ऊरक, लगाश तथा निप्पुर आदि थे।
० प्रो. श्रीराम गोयल ने सुमेरियन सभ्यता को ‘पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं का जनक’ माना है।
० 1929 ई. एंग्लोअमेरिकन अभियान दल के प्रो. वूली द्वारा किए गये ‘उर’ नगर के उत्खनन से सुमेरियन सभ्यता पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।
० 3200-3100 ई. पू. में दक्षिण मेसोपोटामिया में विकसित होने वाली शहरी बस्तियों को प्रसिद्ध विद्वान गॉर्डन चाइल्ड ने ‘शहरी क्रान्ति’ का नाम दिया है।
० मेसोपोटामिया की कांस्ययुगीन सभ्यता के क्रम में 5000 से 2350 ई. पू. के कालखंड को पूर्व राजवंश काल माना है। इस दौरान उर, उरक, किश, लगाश, आदि नगर राज्यों में आपसी संघर्ष हुआ।
० लुगल जागेशी एक प्रसिद्ध शासक था जिसने उर तथा उरक पर विजय प्राप्त करके ऐरक को अपनी राजधानी बनाया।
० सारगान ने अक्कदी नगर राज्य को अक्कादी साम्राज्य में बदल दिया।
० सारगोन के शासन काल के दस्तावेजों में बड़े परिसर के मानचित्र को विश्व के प्राचीनतम मानचित्रों में स्थान प्राप्त है। यह मानचित्र गासुर नगर की खुदाई से मिला था।
० 2000 ई. पू. में उर के तृतीय राजवंश का पतन हुआ।
० कांस्ययुगीन सुमेरिया अनेक छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों में बंटा था, जिन्हें ‘नगर-राज्य’ कहते थे।
० नगर राज्यों का शासन नागरिकों की संसद चलाती थी।
० डॉ. श्रीराम गोयल ने सुमेरियन संस्थाओं को विश्व की प्राचीनतम जन सभाएं बताया है।
० पेटसी या एंसी ‘देवता के प्रतिनिधि’ के रूप में नगर राज्य का मुखिया था जबकि राजा को ‘लूगल’ कहा जाता था।
० शुल्गी या ढुंगी की विधि संहिता को विश्व की प्राचीनतम विधि संहिता माना जाता है, जिसके आधार पर हम्बूरावी ने अपनी विधि संहिता तैयार की।
० मंदिर सुमेरियन सभ्यता में सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केन्द्र थे।
० प्राचीन सुमेर का समाज तीन वर्गों उच्च (अभिजात्य), साधारण एवं निम्न वर्ग में बंटा हुआ था।
० रानी शुब-अद की समाधि की खुदाई से अनेक प्रकार के आभूषण मिले हैं, जो सुमेरियन सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं।
० दास प्रथा सुमेरियन समाज का महत्वपूर्ण अंग थी।
० सुमेरियनों ने विश्व के प्रथम कृषि पंचांग का निर्माण किया था।
० सुमेर के लोगों ने विश्व में सबसे पहले सिंचाई की व्यवस्था नहरें खोदकर एवं नदियों पर बांध बनाकर प्रारंभ की थी।
० भार ढोने के लिए पहिये का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम सुमेरियनों ने किया था।
० वस्तु विनिमय में सुमेर के लोग चांदी की छड़ों का प्रयोग करते थे।
० सुमेरियनों ने सर्वप्रथम विश्व में ऋण देने की प्रथा आरंभ की थी।
० अनु, एनलिल, एनकी, पृथिवी, इन्नेनी आदि सुमेर के प्रमुख देवता थे। वहाँ प्रत्येक नगर का अपना देवता होता था।
० पहाड़ियों पर बने सुमेरियन मंदिरों को जिगुरात कहा जाता था।
सुमेरियनों ने कीलाक्षर लिपि का प्रारंभ किया था।
सुमेरियन पाठशाला के प्रधान अध्यापक को उम्मिया कहा जाता था।
० सुमेरियनों ने सबसे पहले मुहावरों तथा कहावतों की रचना की।
‘० उरध्वज’ तथा ‘इयन्नातुम का गृधपाषाण’ मूर्तिकला के महत्वपूर्ण नमूने हैं।
० सुमेर के लोग अंक पद्धति में 100 के स्थान पर 60 का प्रयोग करते थे।
० 2700 ई. पू. में लुलु सुमेर का प्रसिद्ध वैद्य था।
० मेहराब, गुम्बद, स्तंभ तथा कुम्हार के चाक के आविष्कारक सुमेरियन ही थे।