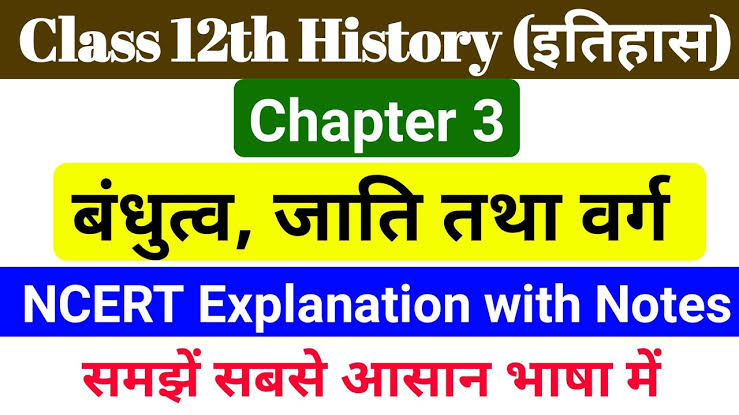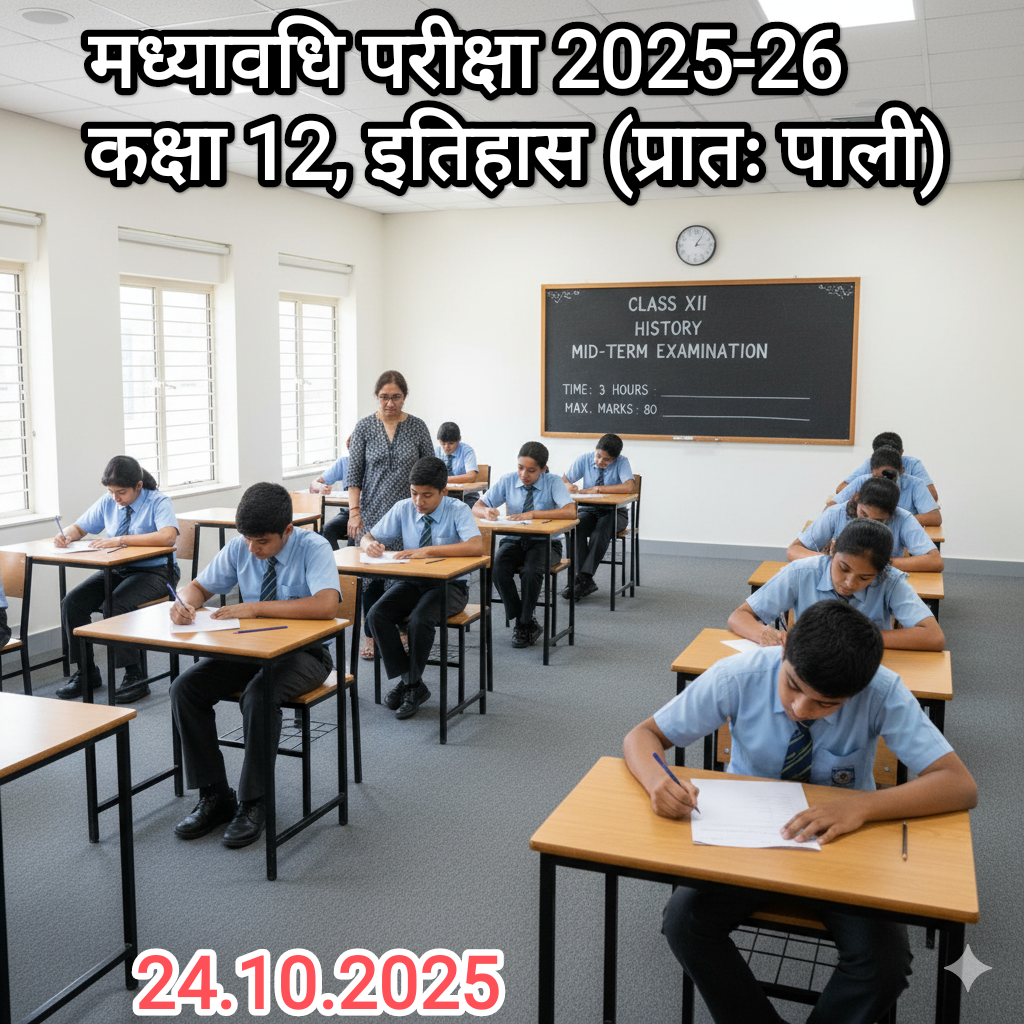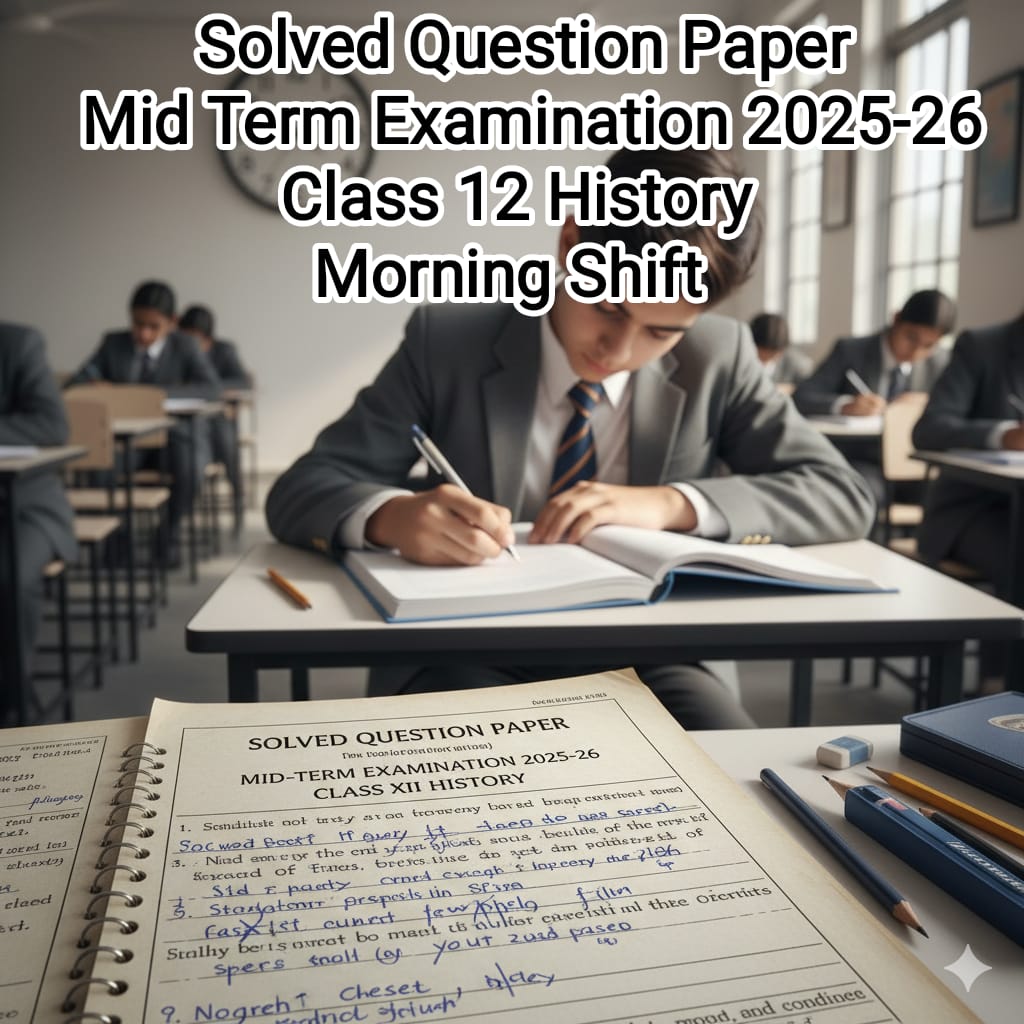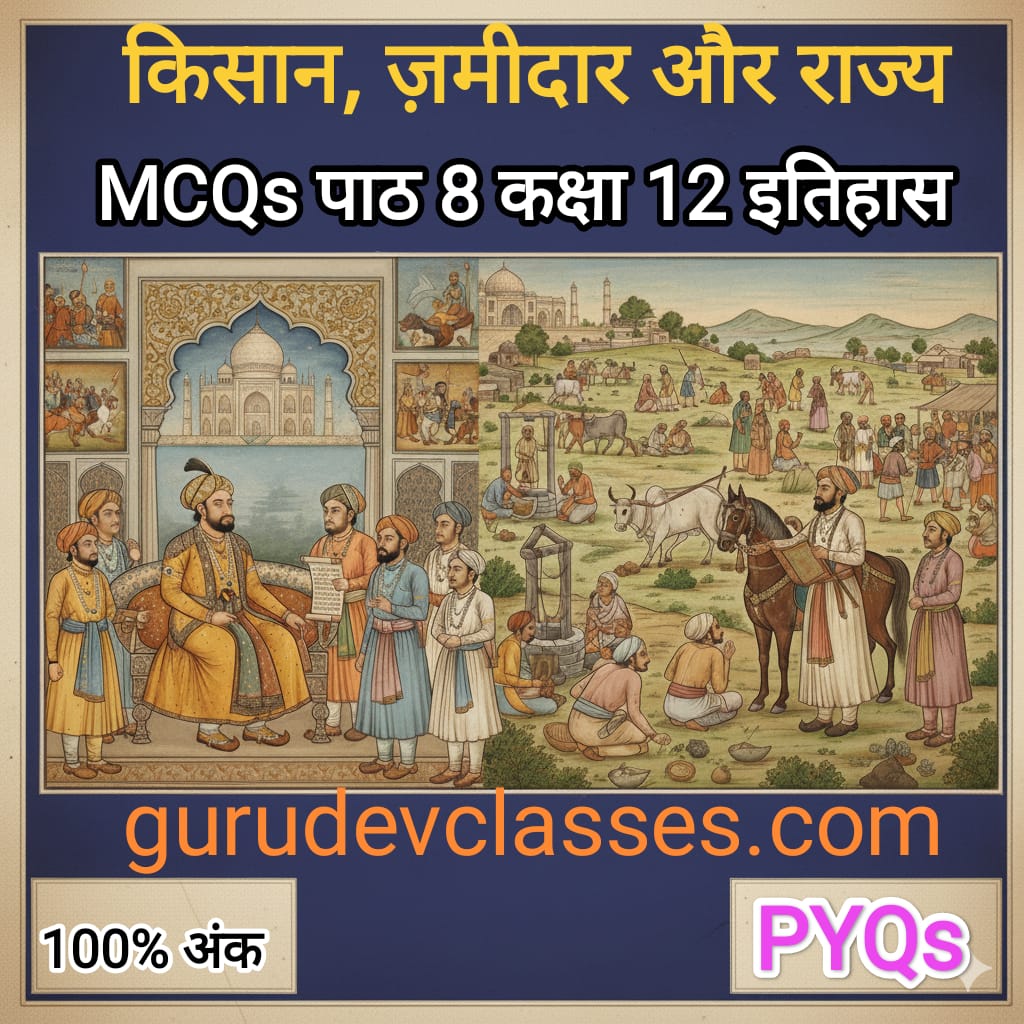- प्रस्तावना
प्राचीन भारतीय समाज में सामाजिक संबंधों (नातेदारी, जाति, वर्ग) की संरचना पर केंद्रित है।
स्रोत: संस्कृत ग्रंथ (विशेषकर महाभारत), शिलालेख, पुरातात्विक साक्ष्य।
- महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण
महाभारत: भारत के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक।
मूल रूप से जय (8,800 श्लोक) → भरत (24,000 श्लोक) → महाभारत (1,00,000 श्लोक)।
500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच संकलित।
संस्कृत में रचित।
इसमें कुरु-पांचाल परिवारों, सामाजिक रीति-रिवाजों और युद्ध की कहानियाँ शामिल हैं।
वी.एस. सुकथंकर द्वारा लिखित आलोचनात्मक संस्करण में “मूल” पाठ प्राप्त करने के लिए बाद में जोड़े गए अंश हटा दिए गए हैं।
- बंधुत्व: रिश्तेदार कौन हो सकता है? बंधुत्व से तात्पर्य रक्त या विवाह पर आधारित संबंधों से है।
पितृवंश: पिता के माध्यम से वंश का पता लगाना (उच्च जाति के हिंदू परिवारों में आम)।
मातृवंश: माता के माध्यम से वंश का पता लगाना (दुर्लभ, जैसे, कुछ दक्षिणी जनजातियों में)।
गोत्र प्रणाली: लगभग 1000 ईसा पूर्व विकसित हुई। ब्राह्मणों के बीच एक पितृवंशीय वर्गीकरण।
नियम: एक ही गोत्र में विवाह करना निषिद्ध था।
बहुविवाह: एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती थीं। पुनर्विवाह: भाई की विधवा से विवाह करना।
- विवाह के नियम
अंतर्विवाह: एक ही समूह/जाति के भीतर विवाह।
बहिर्विवाह: अपने गोत्र या समूह के बाहर विवाह।
ग्रंथों में महिलाओं की भूमिका सीमित थी।
धर्मशास्त्रों जैसे ग्रंथों में विवाह, उत्तराधिकार और नातेदारी के नियम निर्धारित किए गए थे।
कन्यादान: विवाह में पुत्री का दान—एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य।
- जाति: सामाजिक पदानुक्रम
वर्ण व्यवस्था ने समाज को चार वर्णों में वर्गीकृत किया:
ब्राह्मण – पुरोहित और शिक्षक।
क्षत्रिय – योद्धा और शासक।
वैश्य – व्यापारी और कृषक।
शूद्र – सेवक और मजदूर।
ब्राह्मण सर्वोच्च दर्जा प्राप्त थे और उन्हें अधिक पवित्र माना जाता था।
अछूत (अवर्ण) – वर्ण व्यवस्था से बाहर, नीच काम करते थे, भेदभाव का सामना करते थे।
यह व्यवस्था वंशानुगत और पदानुक्रमित थी।
मनुस्मृति ने वर्ण और लिंग-आधारित कर्तव्यों के लिए नियम निर्धारित किए।
- चार वर्णों से परे: जातियाँ
जातियाँ: व्यवसाय के आधार पर उपजातियाँ।
वर्णों की तुलना में अधिक लचीली और स्थानीय।
जातियों के अपने नियम, पंचायतें और पदानुक्रम थे।
- सामाजिक अंतर और गतिशीलता
यद्यपि कठोर, सामाजिक गतिशीलता के कुछ अवसर थे:
शक्तिशाली शूद्र या शासक क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त कर सकते थे।
बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती दी।
सातवाहन और अन्य राजवंशों ने ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों और विवाहों का समर्थन करके शासन को वैध बनाने का प्रयास किया।
- लैंगिक और सामाजिक भूमिकाएँ
महिलाओं को सार्वजनिक अनुष्ठानों और उत्तराधिकार से काफी हद तक बाहर रखा गया था।
लेकिन विवाह के माध्यम से वंश, संपत्ति और संबंध निर्माण में उनकी भूमिका आवश्यक थी।
उच्च जातियों में विधवा पुनर्विवाह को हतोत्साहित किया जाता था।
कुछ रानियों और राजसी महिलाओं के पास अधिकार थे (जैसे, शिलालेख, दान)।
- महाभारत: एक ऐतिहासिक संसाधन
सामाजिक मूल्यों, राजनीति, नातेदारी आदि को समझने का एक समृद्ध स्रोत।
कहानियाँ प्राचीन भारतीय समाज के वास्तविक और आदर्श व्यवहार को दर्शाती हैं।
परिवारों के भीतर संघर्ष, जातिगत कर्तव्य, युद्ध नैतिकता और महिलाओं की भूमिकाओं को दर्शाती हैं।
द्रौपदी की कहानी लिंग और शक्ति की जटिलताओं को उजागर करती है।
- इतिहासकारों द्वारा महाभारत का प्रयोग
इतिहासकार इसका आलोचनात्मक प्रयोग करते हैं: तथ्य, विश्वास और बाद में जोड़े गए अंशों के बीच अंतर करते हैं।
वी.एस. सुकथंकर के आलोचनात्मक संस्करण ने मूल पाठ को छानने में मदद की।
महाकाव्य समय के साथ सामाजिक मूल्यों में बदलाव दर्शाता है।
- इस अध्याय में प्रयुक्त स्रोत
ग्रंथ: महाभारत, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण।
शिलालेख और पुरातत्व: सातवाहन शिलालेख, मंदिर दान।
महाकाव्यों की टिप्पणियाँ और बाद के संस्करण।
महत्वपूर्ण बिंदु
पितृवंश: पुरुष वंश के माध्यम से उत्तराधिकार।
गोत्र: पिता के माध्यम से ज्ञात कुल।
कन्यादान: विवाह में पुत्री का दान।
धर्मशास्त्र: हिंदू कानूनी और नैतिक ग्रंथ।
जाति: व्यवसाय पर आधारित उपजाति।
अंतर्विवाह/बहिर्विवाह: समूह के भीतर/बाहर विवाह करना।
महाभारत: प्रारंभिक भारतीय समाज का महाकाव्य स्रोत।
निष्कर्ष
महाभारत प्रारंभिक भारतीय समाज, उसकी जटिल नातेदारी संरचनाओं, जातिगत पदानुक्रमों और लैंगिक भूमिकाओं की एक झलक प्रदान करता है।
यद्यपि ये ग्रंथ निर्देशात्मक हैं, फिर भी इनमें सामाजिक लचीलेपन और प्रतिस्पर्धा के संकेत मिलते हैं।